01 Nov वर्टिकल फार्मिंग: कृषि का भविष्य
Vertical Farming: Future of Agriculture
फसलों को क्षैतिज खेती के बजाय ऊर्ध्वाधर सतहो (जैसे दीवारों, शेल्फ या ऊर्ध्वाधर संरचना ) पर उगाना वर्टीकल फार्मिंग कहलाता है, वर्टिकल डिजाइन द्वारा भूमि के उपयोग को अधिकतम करने के लिए इस प्रकार की खेती प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग की अवधारणा 1999 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रोफेसर डिक्सन डेस्पोमियर द्वारा प्रस्तावित की गई थी। भारत में 21 वीं शताब्दी के दूसरे दशक में वर्टिकल फार्मिंग शुरू की गई है।
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इस तकनीक को अधिक अनुकूल एवं लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसन्धान एवं प्रचार-प्रसार पर काम कर रहा है। आधुनिक वर्टिकल खेती की सुविधाएं परिष्कृत सेंसर और जलवायु नियंत्रण प्रणालियों के साथ प्रकाश, आर्द्रता, तापमान और पोषक तत्वों को विनियमित कर सकती हैं।

वर्टिकल खेती का मुख्य उद्देश्य नवीनतम तकनीक जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी खेती करने की प्रणाली का अनुकूलन करना है। वर्टिकल कृषि प्रणालियों के लिए संरचनाओं के कुछ सामान्य विकल्पों में इमारतें, शिपिंग कंटेनर, सुरंगें और पीवीसी पाइप से बनी संरचनाये शामिल हैं।
पारम्परिक तरीके से एक ही स्तर पर सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की खेती करने के बजाय, यह विधि लंबवत खड़ी परतों में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है।
वर्टिकल खेती की आवश्यकता:
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक आबादी 2050 तक 10 बिलियन तक पहुंचने के आसार है और जिसके भरण पोषण के लिए 70% अतिरिक्त खाद्दान की आवश्यकता है। इसलिए, खेती की प्रक्रिया में नई तकनीकी की आवश्यकता है और वर्टिकल खेती उन नई तकनीकी में से एक है तथा कम स्थान में अधिक भोजन का उत्पादन करने का एक प्रभावी तरीका है। वर्टिकल खेती के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है :
1 भविष्य के लिए तैयारी:
2050 तक, दुनिया की लगभग 80 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है, और बढ़ती आबादी से भोजन की मांग में बढ़ोतरी होगी तथा साथ ही शहरीकरण, औद्योगीकरण, सड़को व अन्य निर्माण कार्यो के कारण खेती योग्य भूमि लगातार काम हो रही है। वर्टिकल खेती का कुशल उपयोग शायद इस तरह की चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
2 सिमित जगह से अधिकतम फसल उत्पादन:
वर्टिकल खेती प्रणाली के द्वारा, सीमित क्षेत्रफल से हम अधिक फसलों का उत्पादन लिया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, वर्टिकल खेती प्रणाली 1 एकड़ क्षेत्र कम से कम 4-6 एकड़ बाहरी क्षमता के बराबर उत्पादन लिया जा सकता है।
3 खेती में पानी का कम उपयोग:
वर्टिकल खेती में सामान्य खेती की तुलना में 70-95 प्रतिशत कम पानी के साथ फसलों का उत्पादन किया जा सकता है।
4 प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित नहीं:
सामान्य खेती प्रणाली में फसलें प्राकृतिक आपदाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं जैसे कि मूसलधार बारिश, चक्रवात, बाढ़ या गंभीर सूखे – जो कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप एक आम बात हैं। इनडोर वर्टिकल विधि द्वारा खेती करने पर प्रतिकूल मौसम के दुष्प्रभाव की संभावना कम होती है, जिससे पूरे वर्ष में अधिक निश्चितता के साथ फसल उत्पादन किया जा सकता है।
5 जैविक खेती के उत्पादन में वृद्धि:
रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग के बिना अच्छी तरह से इनडोर वातावरण में फसलों का उत्पादन किया जाता सकता है, वर्टिकल खेती हमें कीटनाशक-मुक्त एवं जैविक खेती प्रणाली द्वारा फसलों का उत्पादन किया जा सकता है।
6 प्रति यूनिट अधिक उत्पादकता:
पारंपरिक खेती में, एक समय में केवल एक फसल का उत्पादन किया जा सकता है, जबकि वर्टीकल फार्मिंग प्रणाली में, कुशल एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके, कई प्रकार की फसलों को अलग -अलग मंजिलों पर एक साथ उत्पादित किया जा सकता है। जिसमे प्रति यूनिट क्षेत्र अधिक उत्पादन लिया जा सकता है ।
वर्टिकल खेती में प्रक्रिया शामिल तकनीक:
वर्टिकल खेत अलग-अलग आकार में आते हैं, सरल दो-स्तरीय या दीवार-माउंटेड सिस्टम से लेकर कंटेनर खेती प्रणाली शामिल है। लेकिन सभी वर्टिकल खेत पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए तीन मिट्टी से मुक्त प्रणालियों में से एक का उपयोग करते हैं: हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, या एक्वापोनिक। निम्नलिखित जानकारी इन तीन बढ़ती प्रणालियों का वर्णन करती है:
1- हाइड्रोपोनिक्स:
यह मिट्टी के बिना फसल उत्पादन की तकनीक है। इस प्रणाली में, फसल के पौधों की जड़ें पोषक तत्वों के घोल में जलमग्न होती हैं, जिसमें मुख्य पोषक तत्व के साथ -साथ आवशयक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं।
कुछ अन्य सामग्रियों का उपयोग पौधों की जड़ों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जाता है जैसे- कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, क्लेबॉल इत्यादि जिसमे पोषक तत्व की आपूर्ति की जाती है और तरल पोषक तत्व मिश्रण को चलाने में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक पंपिंग सिस्टम द्वारा समय-समय पर पुनर्नवीनीकरण किया जाता है।
यह रोगों, कीटों कीटों या अन्य खरपतवार से मुक्त उपज देता है। हाइड्रोपोनिक्स में प्रति यूनिट क्षेत्र में उच्च उपज शामिल है और खेती की अन्य पारंपरिक प्रणाली की तुलना में पानी के उपयोग को कम करता है।
2- एक्वापोनिक्स:
एक्वापोनिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है: एक्वाकल्चर, जो मछली की खेती और हाइड्रोपोनिक्स – मिट्टी के बिना फसल पौधों की बढ़ती तकनीक को संदर्भित करता है।
इसका अर्थ है एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जलीय जीवों (मछली) को रखना एवं उत्पादन लेना। इसमें बिना किसी अतिरिक्त खाद अथवा रासायनिक उर्वरक के केवल मछली अपशिष्ट से ही खेती की जाती है।
3- एरोपोनिक्स:
एरोपोनिक्स मिटटी के बिना पौधो को उगाने की एक तकनीक हैं। इस विधि में को पौधों के बढ़ने के लिए किसी भी ठोस या तरल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें पौधो की जड़ो को हवा में लटकाया जाता है तथा नियमित रूप से पोषक तत्वों से भरपूर घोल से छिड़काव किया जाता है।
एरोपोनिक्स एक आधुनिक एवं सबसे टिकाऊ तकनीक है जो अन्य खेती तकनीकों की तुलना में 90% कम पानी का उपयोग करती है तथा ऊर्जा की बचत करती है। ऑक्सीजन की आवश्यक उपलब्धता के कारण पौधों की वर्द्धि एवं विकास अच्छी प्रकार से होता है तथा उपज में भी वर्द्धि होती है।
वर्टिकल खेती संरचना का प्रकार
बिल्डिंग आधारित फार्म:
बहुमंजिला इमारतों को अक्सर वर्टिकल खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि, नयी बिल्डिंग का निर्माण कभी -कभी घर के वर्टिकल खेती प्रणालियों के लिए भी किया जाता है।
शिपिंग कंटेनर:
शिपिंग कंटेनर भी वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम के लिए बहुत लोकप्रिय विकल्प हैं। शिपिंग कंटेनर विभिन्न प्रकार के पौधों को बढ़ाने के लिए मानकीकृत, मॉड्यूलर केबिन के रूप में काम करते हैं, और प्रकाश व्यवस्था, लंबवत स्टैक्ड हाइड्रोपोनिक्स, स्मार्ट जलवायु नियंत्रण और निगरानी प्रणालियों से सुसज्जित होते हैं।
वर्टिकल फार्मिंग में प्रयुक्त मीडिया
परलाइट:
ज्वालामुखीय चट्टान के अति गर्म होने के बाद उत्पन्न विस्तारित क्रिस्टल कणों को परलाइट के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मिट्टी के घनत्व को कम करने और जल निकासी में सुधार करने के लिए गमलों में मिट्टी के मिश्रण में किया जाता है। सामान्यतः, परलाइट में वायु-जल अनुपात अधिक होता है तथा जड़ क्षेत्र में वायु संचार को बढ़ाता है।





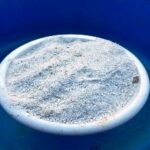
वर्मी कुलाइट:
यह खनिजों के स्मेक्टाइट समूह का सदस्य है, जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। यह अपने वजन का 3-4 गुना पानी को धारण रखने की क्षमता रखता है और साथ ही मिट्टी की जल निकासी और वायु संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है।
कोकोपीट:
अल्ट्रापीट, नारियल कॉयर और कोको-टेक इस उत्पाद के कुछ व्यापारिक नाम हैं। यह नारियल के छिलको से बना एक प्राकृतिक फाइबर पाउडर होता है। इसे मिटटी रहित खेती का सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है वर्मीकुलाईट और परलाइट के साथ मिलकर प्रयोग करने पर जड़ो के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। यह एक जैविक उत्पाद है जिसका H. मान 5.2 से 6.8 के बीच होता है तथा यह अपने वजन का 8-9 गुना तक पानी रोक सकता है
पीट मॉस:
पीट मॉस जल धारण करने के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम है। पीट मॉस को आमतौर पर पहले से पैक की गई गमलों की मिट्टी में मिलाकर उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग उन गमलों में किया जाता है, जिन्हें अतिरिक्त नमी की आवश्यकता होती है।
रेत:
पौधों के लिए वृद्धि माध्यम के रूप में रेत का उपयोग लाभदायक है, जिन्हें शुष्क तथा ढीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। गाजर और आलू, सामान्य जड़ वाली फसलें, रेत में बेहतर होती हैं क्योंकि यह छिद्रयुक्त, हल्की होती है, हालाँकि अन्य मीडिया फसलों की तरह अधिक नमी को बरकरार नहीं रखती।
रॉक वूल:
हाइड्रोपोनिकली, रॉक वूल, जिसे खनिज ऊन भी कहा जाता है, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम है। पिघले हुए खनिज यौगिकों के एरोसोलीकरण के परिणामस्वरूप, एक रेशेदार माध्यम बनता है। सूक्ष्मजीवीय क्षरण के प्रति अभेद्य भी है।
वर्टिकल खेती की चुनौतियां
वर्टिकल खेती की तकनीक में बहुत सारे लाभों के साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है जो इस प्रकार है-
1 प्रकाश की चुनौतियां:
इमारतों के भीतर वर्टिकल खेतों में पौधे के विकास के लिए प्राकृतिक प्रकाश की पहुंच कम होती है, इसलिए कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दो-तिहाई से अधिक वैश्विक ऊर्जा शहरों में खपत की जाती है जो कि वर्टीकल फार्मिंग के विरोधियो द्वारा अवसर एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पेश कि जाती है।
2 ऊर्जा की खपत:
स्वस्थ पौधे के विकास के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताएं घर के अंदर, आर्द्रता के साथ-साथ उपयुक्त तापमान भी हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक नियंत्रण और निगरानी की आवश्यकता होती है तथा साथ ही पौधों के लिए उपयुक्त तापमान बनाये रखने एवं कृत्रिम प्रकाश वयवस्था के लिए उच्च ऊर्जा कि आवश्यकता होती है।
3 पानी की मांग की एवं उपलब्धता:
इस प्रणाली का एक प्रमुख कारक पानी का परिवहन है, विशेष रूप से ऊंची इमारतों में में उच्च भार के साथ पानी कि आपूर्ति एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
4 तकनिकी ज्ञान की आवश्यकता:
वर्टीकल फार्म के संचालन एवं प्रबंधन के लिए उच्च स्तर के तकनिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से प्रकाश वयवस्था , जलवायु नियंतरण एवं पोषक तत्व प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में।
5 उच्च पारंभरिक लागत:
किसी भी वर्टीकल फार्म को स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचे, मशीनरी, उपकरण एवं तकनिकी सहित उच्च अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है।
6 सिमित फसल विविधिता:
पर्याय ऊध्वार्धर खेतो में विभिन प्रकार की फैसले पैदा की जा सकती है लेकिन सभी प्रकार की खाद्यान फैसले इस प्रणाली द्वारा उगने के लिए उपयुक्त या आर्थिक रूप से वयवहार नहीं हो सकती है।
लेखक:
राज कुमार, रवीना, विकास कुमार शर्मा
पी. ऍफ़. डी. सी., चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा, 125004
ई-मेल: rajkumarhau9@gmail.com

