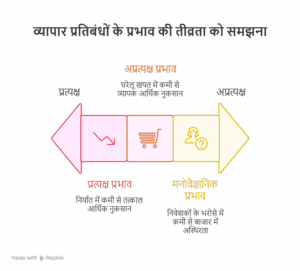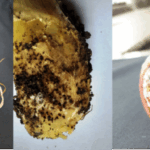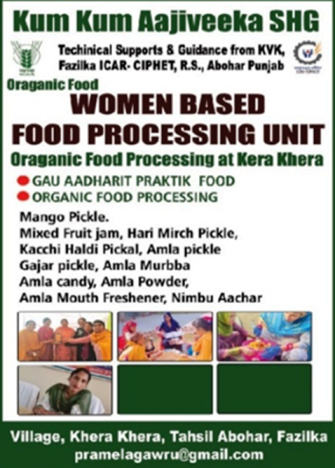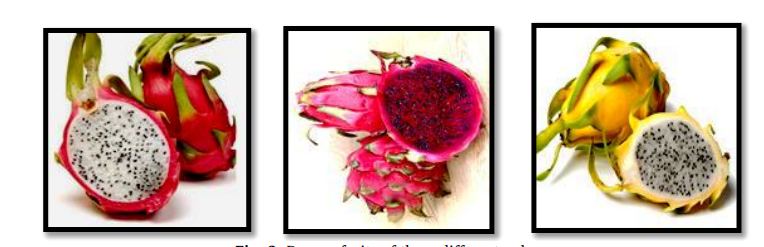29 Oct जैविक विधि द्वारा पादप रोग नियंत्रक
Plant disease control by biological methods
जैविक विधि से पादप रोग नियंत्रण एक ऐसी तकनीक है जिसमें रोगजनकों (जैसे कवक , बैक्टीरिया, वायरस) की आबादी को कम करने या रोकने के लिए प्राकृतिक जीवों (जैसे अन्य सूक्ष्मजीव, कीट, इत्यादि) का उपयोग किया जाता है. यह रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करके, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक सुरक्षित है.
वर्तमान समय मे पादप रोग के प्रबंधन मे विभिन प्रकार के जैव नियंत्रक उपयोग किए जा रहे है और इनकी भूमिका रोगो के उपचार मे बढ़ती जा रही है। इसका एक महत्वपूर्ण करना यह है कि ये जैव नियंत्रक पर्यावरण को नुकसान नही पाहुचते है और मिट्टी कि उर्वरक क्षमता बनाए रखते है।
पादप-रोग, विभिन्न प्रकार के रोगजनको (पथोजेंस) के द्वारा उत्पन्न होते है। ये रोग जनक विषाणु, जीवाणु, कवक विभिन्न प्रकार के कीट इत्यादि हो सकते है।
पादप रोगों का जैविक नियंत्रण:
एक सर्वे के अनुसार सम्पूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 29 हजार करोड़ रुपए तक का नुकसान फसलों पर लगने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से होता है, एवं इसके नियंत्रण हेतु साधारणतया जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनो की खपत लगभग 17.4 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष है, जिसका 90 प्रतिशत भाग कीट, खरपतवार एवं विभिन्न रोगों के रासायनिक नियंत्रण में इस्तेमाल होता है।
एक अनुमान के मुताबिक, इन रसायनों के इस्तेमाल के कारण हजारों करोड़ रुपए की कृषि पैदावार को बाजार में अस्वीकार कर दिया जाता हैं क्योकि ये रासायनिक पदार्थ खाध पदार्थो के द्वारा हमारी खाद्य श्रंखला में चले जाते है जिससे मानव विभिन्न रोगो से ग्रसित हो जाता है। साथ ही साथ ये रसायन मृदा में शामिल होकर हमारे भूजल को भी प्रदूषित कर रहे है।
इस प्रकार इन रसायनो के कुप्रभाव से रोग करको मे रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। इस तरह कुछ मृदा जनित रोगो का नियंत्रण भी रसायनो के द्वारा कठिन होता जा रहा है। अतः रासायनिक पदार्थो के बढ़ते हुए दुष्प्रभावों को कम करने के लिये एक विकल्प के रूप में जैविक पादप रोग नियंत्रण की महत्त्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समय मे उभर कर आ रही है।
जैव नियंत्रण
जैविक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसमे पौधो मे रोग/ रोग कारको के नियंत्रण के लिये दूसरे जीवों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक से अधिक सूक्ष्मजीवियों का उपयोग भी रोग कम करने या रोकने के लिये किया जा सकता है। अतः वे सूक्ष्मजीव जो विभिन्न रोगों के नियंत्रण के लिये प्रयुक्त होते हैं, जैविक रोगनाशक कहलाते हैं।
रोग नियंत्रण की इस प्रक्रिया मे, ये सूक्ष्मजीव रोग कारकों की संख्या को कम कर देते है तथा उनकी व्रद्धि को रोक देते है जिससे संक्रमण के बाद बीमारी अधिक संक्रामक नही हो पाती और धीरे-धीरे सम्पूर्ण रोगों का नियंत्रण हो जाता है।
जैविक नियंत्रण में कवक एवं जीवाणु दोनों प्रकार के जैविक रोग नाशक सूक्ष्मजीव प्रयोग में लाये जा रहें इनमें ट्राइकोडर्मा हारजिएनम, ट्राइकोडर्मा विरिडि, एसपरजिलस नाइजर, बैसिलस सबटिलिस एवं स्यूडोमोनास फ्लोरेसेन्स प्रमुख हैं।
जैव नियंत्रक के प्रमुख गुण एवं महत्व:
- इनको भंडारण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरण किया जा सकता है।
- इनका बड़े पैमाने पर पालन किया जा सकता है तथा एकीकरण किया जा सकता है।
- इनको प्रयोगशाला मे आसानी से तैयार किया जा सकता है।
- इनकी अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन क्षमता होती है अतः अधिक मात्रा मे उत्पादन किया जा सकता है।
- ये बड़े क्षेत्रों मे उपस्थित कीटो या रोग जनकों के नियंत्रण मे सक्षम होते है।
- जैविक एजेंट में रोग नियंत्रक की अत्यधिक विस्तृत क्षमता होती हैं।
- ये रोग नियंत्रण की वैकल्पिक विधि हैं ।
- इसके जैव उत्पाद की क्षमता बहुत विस्तृत, स्थिर और सरल होती है। विकसित प्रजातियाँ 10-45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 8 प्रतिशत नमी पर स्थिर रहती है।
- मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।
- मृदा में कोई प्रदूषण नहीं होता है, मृदा में रहने वाले अन्य लाभदायक जीवों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।
- प्रभावी लागत भी कम आती है ।
- जैविक नियंत्रण का दीर्घकालिक प्रभाव होता है ।
जैव नियंत्रक और प्रयोग करने की विधियाँ
टूइकोडरमा विरीडी/ट्राइकोडरमा-हारजिएनम
टुइकोडरमा फफूंदी पर आधारित घुलनशील जैविक फफूंदीनाशक है। ट्राइकोडरमा विभिन्न प्रकार के फसलों, फलों एवं सब्जियों में जड़ सड़न, तना सड़न, डैम्पिंग ऑफ, उकठा, झुलता आदि फफूंदजनित रोगों में लाभप्रद पाया गया है। धान, गेंहूँ, दलहनी फसलों, गन्ना कपास, सब्जियों, फलो आदि के रोगों का यह प्रभावी रोकथाम करता है। ट्राइकोडरमा के कवक तंतु हानिकारक फफूंदी के कवकतंतुओं को लपेट कर या सीधे अन्दर घुसकर उसका रस चूस लेते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन स्पर्धा के द्वारा कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ का स्ताव करते हैं, जो बीजों के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाकर हानिकारक फफूँदी से सुरक्षा करते हैं। इसके प्रयोग से बीजों का अंकुरण अच्छा होता है तथा फसलें फफूँदजनित रोगों से मुक्त रहती है। नर्सरी में इसके प्रयोग करने पर बीजों की जमाव एवं वृद्धि अच्छी होती है। इसके प्रयोग से पहले एवं बाद में रासायनिक फफूँदीनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ट्राइकोडरमा की सेल्फ लाइफ सामान्य तापक्रम पर एक वर्ष होता है।
ट्राइकोडरमा के प्रयोग की विधि
- बीज शोधन हेतु 5 ग्राम टूइकोरडमा प्रति कि०ग्रा० बीज के दर से बीजोपचार कर बुवाई करनी चाहिए।
- कन्द एवं नर्सरी पौधा उपचार हेतु 5 ग्रा0 बनाकर पौधों की जड़ों को सोधित कर बुवाई लीटर पानी की दर से घोल रोपाई करनी चाहिए।
- भूमि शोधन हेतु 5 कि0ग्रा0 / हे0 को लगभग 75 कि० ग्रा० गोबर की खाद में मिलाकर हलके पानी का छींटा देकर 8-10 दिन तक छाया में रखने के उपरान्त बुआई से पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देना चाहिए।
- बहुवर्षीय पेड़ो के जड़ के चारो तरफ 1-2 फीट चौड़ा एवं 2-3 फीट गढढ़ खोदकर प्रति पौधा 100 ग्राम ट्राइकोडरमा को 8-10 कि० ग्रा० गोबर के खान में मिलाकर गढ्ढ़े की भराई करनी चाहिए।
- खड़ी फसल में फफूँदजनित रोग के नियंत्रण हेतु 5 कि० ग्रा० / हे0 क दर से 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर सायंकाल छिड़काव क आवश्यकतानुसार 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा प्रयोग करें।
व्युवेरिया बेसियाना
ब्यूवेरया बैसियाना फफूँद आधारित जैविक कीटनाशक है, जो विभिन्न प्रकार हे फसलों, फलों एवं सब्जियों में लगने वाले फलीभेदक, पत्ती लपेटक, पत्ती खाने वाले कीट, चूसने वाले कीटों, भूमि में दीमक एवं सफेद गरार आदि की रोकथाम के लिए लाभकारी है। ब्यूवेरिया बैसियाना के प्रयोग से पहले एवं बाद में रासायनिक फफूदीनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
प्रयोग की विधि
भूमि शोधन हेतु व्यूवेरिया बैसियाना की 2.5 कि0ग्रा0 / हे० लगभग 75 कि० ग्रा० गोबर की खाद में मिलाकर अन्तिम जुताई के समय प्रयोग करना चाहिए।
खड़ी फसल में कीट नियंत्रण हेतु 2.5 कि० ग्रा० हे0 की दर से 400-500 लीटर पानी में घोलकर सायंकाल छिड़काव करें आवश्यकतानुसार 15 दिन के अंतराल पर दोहराया जा सकता है।
स्यूडोमोनास फ्लोरिसेन्स
स्यूडोमोनास फ्लोरिसेन्स बैक्टीरिया आधिरित जैविक फफूंदीनाशक /जीवाणुनाशक है जो विभिन्न प्राकर के फसलों, फलों, सब्जियों एवं गन्ना में जड़ सड़न, तना सड्न, डैम्पिंग ऑफ, उकठा, लाल सड़न, जीवाणु झुलसा, जीवाणुधारी आदि फफूँदजनित एवं जीवाणुजनित रोगों के नियंत्रण के लिए प्रभावी पाया गया है।
प्रयोग विधि
बीज शोधन हेतु 10 ग्राम स्यूडोमोनास को 15-20 मि० ली० पानी में घोल बनाकर एक कि० ग्रा० बीज को उपचारित कर छाया में सुखने के उपरान्त बुवाई करना चाहिए।
ब्बा भूमि शोधन हेतु 2.5 कि० ग्रा० स्यूडोमोनास / हे0 10-20 कि० ग्रा० महीन पिसी हुई बालु में मिलाकर बुवाई से पूर्व उर्वरकों की तरह छिड़काव करना लाभप्रद होता है।
मेटाराइजियम एनिसोप्ली
मेटाराइजियम एनिसोप्ली फफूँद आधारित जैविक कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार के फसलों, फलों एवं सब्जियों में लगने वाले फली भेदक, पत्ती खाने वाले कीट, चूसने वाले कीट, भूमि में दीमक एवं सफेद गाजर आदि के रोकथाम के लिए लाभकारी है। मेटाराइजियम एनिसोप्ली कम आर्द्रता एवं अधिक तापक्रम पर अधिक प्रभावी होता है।
प्रयोग विधिः-
व्यूवेरिया बैसियाना के समान प्रयोग करें।
वर्टीसिलियम लैकानी
वर्टीसिलियम लैकानी फफूँद आधारित जैविक कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार के फसलों में चूसने वाले कीटों, माहु, थ्रिप्स, जैसिड, के रोकथाम के लिए लाभकारी है। इसके प्रयोग के 15 दिन पहले एवं बाद में रासायनिक फफूँदीनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
प्रयोग विधिः-
खड़ी फसल में कीट नियंत्रण हेतु 2.5 किर) ग्रा० प्रति हे0 की दर से 400-500 लीटर पानी में घोलबनाकर छिड़काव करें तथा आवश्यकतानुसार 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें।
बैसिलस यूरिनभियंन्सिस (बी० टी०)
वैसिलस थुरिनजियेन्सिस बैक्टीरिया आधारित जैविक कीटनाशक है। वैसिलन धूरिनजियेन्सिस प्रजाति कुटकी, 05 प्रतिशत डब्लू) पी० विभिन्न प्रकार के फसलों, सब्जियों एवं फलों में लगने वाले लेपिडोप्टेरस कुल के फली भेदक, पत्ती खाने वात कीटों की रोकथाम के लिए लाभकारी है। इसके प्रयोग के 15 दिन पूर्व या बाद में रासायनिक बैक्टेरीसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
प्रयोग विधिः-
खड़ी फसल में कीट नियंत्रण हेतु 0.5-1.0 कि० ग्रा० प्रति हे0 की दर से 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें आवश्यकतानुसार 15 दिनों के अंतराल पर सार्थकाल में छिड़काव करना चाहिए।
न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वाइरस (एन.पी.भी.)
यह एक प्रकार का विषाणु है जो कि स्पेसिज विशेष होता है। चना की सुंडी एवं तम्बाकू की सूंडी से बना हुआ ए० पी० बी० चने की सूंडी पर ही काम करता है। कॉट की सूडी के द्वारा वाइरस युक्त पत्ती या फली खाने के 3 दिन बाद सूडियों का शरीर पीला पड़ने लगता है तथा एक सप्ताह के बाद सूंडिया काले रंग का होकर मर जप्ती
नीम उत्पादों का प्रयोग
निम्बोली (बीज) का उपयोगः
नीम के पके फलों का छिलका उतारकर बीजों को सुखाकर कूट कर बारीक पाउडर बना लेते है। अब 20 कि० ग्रा० पाउडर को 40 लीटर पानी में 12 घंटे के लिए भिगोते हैं। तत्पश्चात छनित पदार्थ को 350 लीटर पानी प्रति हे0 की दर से मिलाकर छिड़काव देर शाम या सुबह को करने से कई प्रकार के कीट व जीवाणुओं से फसल की सुरक्षा होती है। 5-7 दिन के अन्तराल पर छिड़काव दोबारा करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके प्रयोग से कीट उसी समय नहीं मरते है ये खाना छोड़ देते है। अण्डे देने की क्षमता में गिरावट आती है तथा उनकी बढ़वार रूक जाती है। इस प्रकार उन पर धीरे-धीरे नियंत्रण हो जाता है। 3 माह पुरानी तक निम्बौली उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा शुद्ध नीम बीज पाउडर 1 कि० ग्रा० मात्रा 50 कि० ग्रा० यूरिया के साथ मिलाने पर पौधों को अधक नाइट्रोजन मिलती है और यूरिया की क्षमता बढ़ जाती है।
नीम का तेलः-
तेल का उपयोग पौधों के रस चूसने वाले कीटों (चेपण, सफेदमक्खी, तेलिया इत्यादि) व लड़ियों की रोकथाम कर फसल को पत्ती संकुचन व मोजेक रोग से बचाया जा सकता है। इसके अलावा सूडियों के नियंत्रण के लिए भी नीम तेल का उपयोग किया जा सकता है। 5 मिलीलीटर नीम तेल तथा। ग्राम कपड़े धोने वाली इजी सर्फ को। लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम के लिए 4 लीटर नीम तेल प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग बीज को दीमक से बचाने के लिए प्रति कि० ग्रा० बीज को 10 मि० ली। नीम तेल से उपचारित करें।
नीम का पत्तीः-
कीटनाशक बनाने के लिए नीम की पत्ती का भी उपयोग किया जा सकता है। 10 कि० ग्रा० नीम की पत्ती को 10 लीटर पानी में डालकर तब तक उबालते रहें जब तक पानी 3 लीटर न हो जाए। ठण्डा होने पर 50 ग्राम डिटरजेन्ट पाउडर अच्छी तरह मिलाकर बारीक कपड़े से छान लेते हैं। अब इस छनित द्रव में से 500 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर पौधा पर छिड़काव करते हैं।
फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग
फेरोमोन ट्रैप कीट प्रबन्धन का एक ऐसा उपाय है जिसमें मादा पतंगे द्वारा नर पतंगे को आकर्षित करने के लिए तोड़े जाने वाली गंध को कृत्रिम रूप से तैयार कर उपयोग में लिया जाता है। इस गंध को सुंघकर नर पतंगे मादा पतंगे की उपस्थिति समझ इसमें आकर फंस जाते हैं। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रथम तो खेत में कीट की उपस्थिति का पता लगाने व दूसरा अधिक मात्रा में नर पतंगो को आकर्षित कर उन्हें नष्ट करने हेतु ताकि नर व मादा के अनुपात को कम किया जा सके। जिससे अण्डे व कीड़े पैदा न कर सके।
फेरोमोन ट्रैप को फसल की ऊँचाई से लगभग 2 फीट ऊपर डंडे के सहारे बाँध देते हैं। हानिकारक पतंगो की उपस्थिति का पता करने के लिए 5-6 ट्रैप तथा अधिक से अधिक संख्या में नर कीट पतंगो को पकड़ने के लिए 15-20 ट्रैप हेक्टेयर की दर से लगाया जाता है।
Authors:
मुकेश कुमार, डॉ. प्रिंस कुमार गुप्ता, डॉ. देवांशुदेव,
सहायक प्रोफेसर सह-जूनियर-वैज्ञानिक, पादप रोगविज्ञान विभाग
डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय अर्राबाड़ी, किशनगंज, बिहार, 855 107
(बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर)
Email : mukeshkumar123450@gmail.com
Related Posts
………………………………………
Related Posts