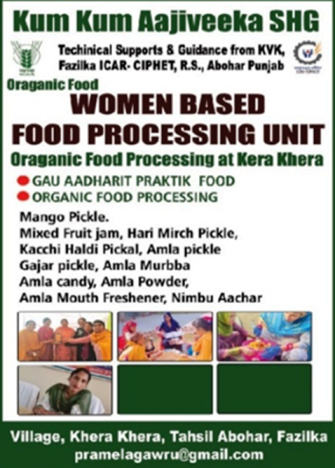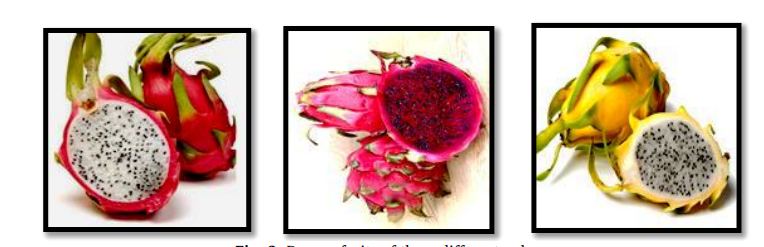21 Nov रबी की फसलों में रोग व्याधियों की पहचान एवं प्रबंधन
Identification and management of diseases in Rabi crops
Based on the initial symptoms of diseases in plants, it is not known whether the disease in the crop is bacterial, viral or due to some other reason. Sometimes disease like symptoms are seen in the plant due to deficiency of any essential element, hence it is important to understand whether the special symptoms displayed by the plant are due to deficiency of any essential element or due to disease.
Identification and management of diseases in Rabi crops
अक्सर पौधों में बीमारियों का शुरुआती लक्षणों के आधार पर पता नहीं लगता है कि फसल में कौन सी बिमारी है। वह बैक्टीरिया जनित है, वायरस जनित है या फिर यह किसी अन्य कारण से है । कभी कभी किसी आवश्यक तत्व की कमी के कारण भी पौधे में बिमारी जैसे लक्षण दिखते हैं अतः यह समझना आवश्यक है की पौधे द्वारा प्रदर्शित किए गए विशेष लक्षण किसी आवश्यक तत्व की कमी कि वजह से है या फिर बिमारी की वजह से।
ये भी देखा गया है कि जानकारी के अभाव में कई बार किसानों के द्वारा अनावश्यक कीटनाशकों के स्प्रे कर दिए जाते हैं जिससे किसानों की अनावश्यक लागत बढ़ जाती है अगर हम मनुष्य एवं पौधों की बात करें तो मनुष्य एक बार बीमार होने के बाद रिकवरी कर लेता है परन्तु पौधों पर बिमारी आने के बाद बिना प्रभावी प्रबंधन के रिकवरी करना मुश्किल होता है जिससे पौधे की मृत्यु हो जाती है
रोग की सही जानकारी न होने की वजह से किसानों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है एवं अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरण भी असंतुलित हो जाता है इसके साथ ही मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है एवं मृदा में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है इस तरीके से किसान को अप्रत्यक्ष रूप से भी नुकसान का सामना करना पड़ता है
अतः इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए उत्तम प्रबंधन आवश्यक है एवं उत्तम प्रबंधन हेतु रोगों और रोग कारकों की पहचान आवश्यक है जिससे कि पौधों पर फाइटो टॉक्सिसिटी को भी कम किया जा सके
पादप रोगों की पहचान के समय ध्यान रखने बातें
हम जानते हैं कि बिमारी फैलने के लिए सामान्यतः तीन कारक जिम्मेदार होते हैं : सहनशील किस्म, रोगकारक की उग्रता, अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थिति। इन तीन कारकों के मिलने से बिमारी उत्पन्न होती है।
हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति में हर चीज को समय के साथ बनाया है जैसे खरीफ समय की बिमारी रबी समय में नहीं आती ठीक उसी प्रकार रबी समय की बिमारी खरीफ में नहीं आती इसके अतिरिक्तत गेहूं की बीमारियां चावल फसल पर नहीं आती , आलू की बीमारियां बैंगन पर नहीं आती।
इसीलिए रोगों की पहचान से पहले हमें फसल एवं फसल में लगने वाले रोगों के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने पर उनके लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं जिनकी आधार पर हम ये जान सकते हैं की रोग विषाणुजनित है बैक्टीरिया जनित है फफूंद जनित है या फिर किसी अन्य कारण से।
रोग की पहचान करते समय पर्यावरण में दिन का तापमान रात का तापमान एवं आद्रता के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि रोग के आने से पहले उसमें रोगकारक के प्रथम स्रोत का अहम योगदान रहता है जैसे कि ऊसपोर, क्लेमाइडोसपोर, कोनिडिया या फिर बीज एवं भूमि जनय रोगकारक ।
यह भी देखा गया है कि खेत में पिछले सीजन में बिमारी थी उस खेत में अगले सीजन में भी वही फसल बोने पर बिमारी के आने की संभावना बढ़ जाती है उदाहरण के लिए चने का उख्टा, धनिये में स्टेम गोल, सरसों में स्टेम रोट इत्यादि।
संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो किसी भी रोग कारक की पहचान के समय पौधे की सहनशील किस्म , रोंग करने वाले रोगकारक की प्रकृति एवं कौन सी पर्यावरणीय परिस्थितियां रोग को अधिक मात्रा में फैलाने में सहायक है के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है।
पहचान करने की आसान विधिया
रोगों की पहचान कई तरीके से किया जा सकता है जिसमें कुछ वैज्ञानिक विधिया भी सम्मिलित है
रोगों के लक्षणों के आधार पर –
बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिनका पौधे पर लक्षणों के आधार पर बिमारी का पता लगाया जा सकता है उदाहरण के लिए चने की उखटा रोग में पौधे पीले पड़ने लगते हैं और ऊपर से नीचे की ओर पत्तियाँ सूखने लगती है एवं अंत में पौधे सूखकर मर जाते हैं इसी तरह अरहर के उखटा रोग में रोगी पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है तथा पौधे मुरझा कर सूख जाते हैं एवं पौधे के तने का निचला भाग काला पड़ जाता है ‘
आलू के पछेती अंगमारी बिमारी पत्तियों पर किनारे वाले भाग पर भूरे धब्बे शुरू होकर पौधे के अन्य भागों पर फैल जाते हैं एवं अनुकूल परिस्थितियों में पौधों का संपूर्ण भाग नष्ट हो जाता है ,
बैंगन एवं टमाटर के मलानी रोग में पानी की कमी न होने पर भी पौधे मुरझा कर सूख जाते हैं एवं जड़ें काली हो जाती है
इसी तरह बहुत सारी बीमारियों का लक्षणों के आधार पर पता लगाया जाना संभव है परन्तु बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका लक्षणों के आधार पर सही रोगकारक एवं सही रोग का पता लगाना संभव नहीं है इस हेतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा या आण्विक स्तर पर रोगकारक का पता लगाया जाता है
सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा –
रोग कारक को पहचानने का प्रयोगशालिक विधि है लेबोरेटरी में सूक्ष्मदर्शी द्वारा रोग कारकों को उनके वास्तविक आकार से कई 1000 गुना बड़ा करके देखा जाना संभव है जिससे कि रोगकारक को पहचानने के लिए काफी बेहतर परिणाम मिलते हैं
आणविक विधियों द्वारा –
आणविक विधियों का प्रयोग करके रोगों की प्रत्यक्ष पहचान की जा सकती है एवं इन विधियों द्वारा स्पीसीज लेवल पर रोक कारकों का पता लगाया जा सकता है। इन विधियों में रोग पैदा करने वाले रोग कारकों जैसे बैक्टीरिया कवक और वायरस का सीधे पता लगाया जाता है ताकि रोग की सटीक पहचान हो सके इसकी कुछ विधिया सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है जैसे पोलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर)।
इस तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से पौधों के रोगजनकों का पता लगाने के लिए किया जाता है पीसीआर तकनीक डीएनए निष्कर्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है एवं यह बैक्टीरिया कवक और वायरल न्यूक्लीक एसिड के आधार पर पौधों की बीमारियों के तेजी से निदान के लिए आवश्यक है
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट विधि –
इस विधि द्वारा एंटीबॉडी और रंग परिवर्तन के आधार पर रोगों की पहचान की जाती है इस पद्धति में वायरस बैक्टीरिया और कवक से लक्ष्य एंटिटी को विशेष रूप से एक एंजाइम संयुग्मित एंटीबॉडी के साथ बांधने के लिए बनाया जाता है एवं इन की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप होने वाले रंग परिवर्तनों के आधार पर रोक कारक का पता लगाया जाता है।
संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो रोगकारक की पहचान सबसे आवश्यक है उदाहरण के तौर पर अगर फसल में बिमारी बैक्टीरियल ब्लाइट है पर पता न लगने के कारण किसान द्वारा फफूंदनाशी का छिड़काव कर दिया जाए तो इससे अनावश्यक लागत के साथ साथ पर्यावरण एवं मिट्टी को भी बहुत अधिक नुकसान होता है अतः बिमारी की सही पहचान जरूरी है
रबी फसलों के प्रमुख रोग
सब्जियों जैसे मिर्च टमाटर बैंगन गोभी इत्यादि को तैयार करने से पहले नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी में आर्द्र गलन रोग सर्वाधिक देखने को मिलता है जो कि फफूंद जनित है इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 प्रतिशत एवं मैनकोजेब 0.2 प्रतिशत या ट्राइकोडर्मा में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।
हमें यह देखने को मिलता है कि नर्सरी में उठी हुई तैयारियों पर नर्सरी तैयार करने से रोग की उग्रता कम होती है एवं इसके साथ ही उस समय पानी का ज्यादा उपयोग न कर के वहाँ कम नमी वाला वातावरण रखने से रोग की तीव्रता कम होती है।
गेहूॅ का आल्टरनेरिया रोग:- यह रोग नमी की अधिकता से उग्र हो सकता है अतः रोग नियंत्रण हेतु मेन्कोजेब 1 से 1.25 किग्रा प्रति हैक्टर छिड़काव करवायें।
गेहूॅ का कण्ड़वा रोग:-इस रोग से बचाव हेतु बुवाई पूर्व बीज उपचार करना चाहिए। अतः गेहँू के बीज को 2 ग्राम बाविस्टिन या 2 ग्राम टेबुकोनाजोल 5.36 प्रतिशत (रेक्सिल) या 2 ग्राम वीटावेक्स प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें।
सरसों की तुलासिता व सफेद रोली:– तुलासिता व सफेद रोली रोगो के प्रथम लक्षण दिखाई देते ही डेढ़ किलो मैंकोजेब प्रति हैक्टर का 0.2 प्रतिशत घोल बना कर छिड़काव करवायें।
सरसों का तना सड़न:- सरसों की पुष्प आने की अवस्था सबसे नाजुक अवस्था है। इस रोग की रोकथाम कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत घोल के छिड़काव से कर सकते है।
धनियां का लोंगिया (स्टैमगाल) रोग:- अगर खेत में लौगियां रोग का इतिहास है तो एवं मौसम में नमी तथा उमस के हो तो रोग की रोकथाम हेतु जल नियंत्रण की सलाह दी जायें। खडी फसल में रोकथाम के लिए बुवाई के 45, 60 एवं 75-90 दिन पर हेक्साकोनाजोल या प्रोपीकोनोजोल नामक दवाई 2 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से अथवा केलेक्जिन / बेलेटान 1 ग्राम प्रतिलीटर पानी के हिसाब से घोल बना कर छिडकाव करें तथा आवश्यकतानुसार छिड़काव दोहरावें।
अफीम का तुलासिता रोग:- तुलासिता रोग से बचाव के लिए मेंकोजेब 0.2 प्रतिशत का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
लहसुन का तुलासिता रोग:- रोग की रोकथाम हेतु मेंकोजेब 0.2 प्रतिशत छिड़काव करने की सलाह दें।
चने का सफेद तना गलन: भूमी के समीप तना सड जाता है व सफेद कवक दिखाई देती है। रोग दिखाई देते ही कार्बेन्डाजिम 0.5 प्रतिशत या बेनोमिल 0.5 प्रतिशत का घोल छिडकाव करे।
आलू का झुलसा: आलू की खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही पहला छिड़काव मैंकोजेब 75 डब्ल्यू.पी. ;2.5 ग्राम प्रति लीटर , दूसरा छिड़काव डाइफेनकानाजोल 25 ई.सी. ;0.5 ग्राम प्रति लीटर, तीसरा छिड़काव मैंकोजेब 75 डब्ल्यू.पी. ; 2.5 ग्राम प्रति लीटर दस दिन के अंतराल पर घोल बनाकर छिड़काव करें।
आलू का तना उत्तक क्षय रोग: इसके कारण तना एवं पर्णवृन्त काले पड़ने लगते हैं। रोगग्रस्त स्थान से तना कठोर पड़ जाता है और थोड़ा सा जोर लगाने से तना आसानी से टूट जाता है, डालियां मुरझाने लगती हैं और पौधे सूखने लगते हैं।
अतः आलू की खड़ी फसल में तना उत्तक क्षय रोग रोग के लक्षण दिखाई देते ही फिप्रोनिल 5ः नामक दवा (15 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में ) या डायफेन्थियुरोन 50 डब्ल्यू.पी. (10 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में ) का छिड़काव करें।
Authors:
डॉ. डी.एल. यादव, निकिता कुमारी एवं निष्ठा मीणा
कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, अनुसंधान निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
Email: dlaau21@gmail.com