09 May शुष्क क्षेत्र में कददूवर्गीय सब्जियों का समेकित कीट प्रबन्धन
Integrated pest management of cucurbits in dry area
कददूवर्गीय सब्जियों को मानव आहार का एक अभिन्न भाग माना जाता है. एक आदमी को रोजाना 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए परंतु भारत मे इसका 1/9 भाग ही मिल पाता है. भारत दुनिया में सब्जी उत्पादन मे दूसरा सबसे बड़ा देश है और चीन का पहला स्थान है. सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों का समृद्ध स्रोत होते हैं. सब्जी उत्पादन में कीडों से बहुत नुकसान होता है. भारत मे कीडों, रोगों, सुत्रकृमियों एवं खरपतवारों से 30% तक नुकसान होता है. कददूवर्गीय सब्जियों में लगने वाले कीट निम्नलिखित है:
कददूवर्गीय सब्जियों मुख्य कीट
1. फल मक्खी:
वैज्ञानिक नाम: बैक्ट्रोसेरा (डैक्स) कुकुरबिटी, कुल: टैफरीटीडी, गण: डीपटैरा
पौषक पौधे: फल मक्खी का आक्रमण सभी कद्दू कुल के पौधो मे होता है जैसे लौकी, करेला, तोरई, कद्दू, ककडी, खरबूज, खीरा, टिंडा आदि.
आर्थिक क्षति एवं नुकसान: इस फल मक्खी के व्यस्क के पंख भूरे रंग के होते है. इस कीट का मैगट ही क्षति पहुंचाता है. इसका प्रकोप फरवरी से लेकर नवम्बर तक होता है. मादा फल मक्खी अपने अंडरोपक को कोमल फलों मे धॅसाकर गूदे मे अण्डे देती है. ग्रसित फल के छेद से लसदार हल्के भुरे रंग का द्रव निकलता है. अण्डे से मैगट निकलते है जोकि गूदे को खाकर उसमें स्पंज, जैसे बहुत से छेद कर देते है ओर फल सडनें लगता है.

कददूवर्गीय फल मक्खी का व्यस्क व शंकु

टिंडे मे फल मक्खी से नुकसान

फुट ककडी मे फल मक्खी से नुकसान

घीया (लौकी) मे फल मक्खी से नुकसान

तोरई(स्पोंजगार्ड) मे फल मक्खी से नुकसान

काचरी मे फल मक्खी से नुकसान

खरबूजें मे फल मक्खी से नुकसान

मतीरें मे फल मक्खी से नुकसान
2. कद्दू का लाल कीड़ा:
वैज्ञानिक नाम: रैफिडोपालपा फोवीकोलीस, कुल: क्राइजोमेलिडी, गण: कोलियोपटेरा
इसकी भारत मे मुख्तया: तीन प्रजातियां पाई जाती है. इनमें से आर. फोवीकोलीस भारत के लगभग सभी राज्यों में पायी जाती है. आर. लैवीसी प्रजाति उत्तरी राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है. और दक्षिण भारत मे आर. सिंकटा अधिक होती है.
पौषक पौधे: इस लाल कीडे का आक्रमण सभी कद्दू कुल के पौधो मे होता है जैसे लौकी, करेला, तोरई, कद्दू, ककडी, खरबूज, खीरा, टिंडा आदि.
आर्थिक क्षति एवं नुकसान: इस कीड़े का व्यस्क एवं ग्रब दोनो नुकसान पहुचाते है. भृंग (व्यस्क) पत्तियों एवं फूलों को नुकसान पहुचाता है और ग्रब पौधे की जडों को खाता है. जो फल जमीन पर रखे होते है उनको इस ग्रब के द्वारा निचले भाग मे छिद्र करके काफी संख्या मे प्रवेश कर जाते है तथा अंदर से खोखला कर देते है.

 कद्दू का लाल कीड़ा ( रैफिडोपालपा फोवीकोलीस)
कद्दू का लाल कीड़ा ( रैफिडोपालपा फोवीकोलीस)
3. हाडा बीटल:
वैज्ञानिक नाम: हैंनोसेपीलेक्ना विजींटिओपंकटाटा, कुल: कोक्सीनेलीडी, गण: कोलियोपटेरा
पौषक पौधे: यह दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में पाया जाता है. यह बैंगन का महत्वपूर्ण कीट माना जाता है, इससे क्षति करीब-करीब सभी सब्जियों मे होती है. जैसे बैंगन, आलु, टमाटर, लौकी, करेला, तोरई, कद्दू, ककडी, खरबूज, खीरा, टिंडा आदि.
आर्थिक क्षति एवं नुकसान: हाडा बीटल के व्यस्क एवं ग्रब दोनो पौधे को नुकसान पहुचाते है. यह एक विशेष तरीके से पत्तियों एवं फलों को कुरेदता है और धीरे धीरे पत्तियों एवं फलों को सुखा देता है.

ग्रब से नुकसान

हाडा बीटल से नुकसान
4.पत्ती भेदक सुंडी:
वैज्ञानिक नाम: डाईफेनिया इंडिका , कुल: पाईरेलिडी , गण: लेपिडोप्टेरा
पौषक पौधे: खीरा, लौकी, करेला, सेम, अरहर, तरबूज, खरबूज, टिंडा, ककड़ी, कद्दू, लोबिया आदि.
आर्थिक क्षति एवं नुकसान: इस कीट की सुंडी ही पौधे की पत्तियों को नुकसान करती हैं. अंडे सें निकलने के बाद सुंडी रेशमी धागे के साथ पत्तियों को रोल करती है और सिराओं के बीच से पत्ती को खाती है. इस कीट की सुंडी फूल एवं फलों को भी नुकसान पहुंचाती है. नुकसान किये हुये फल बाद में सड़ने लगते है.

सुण्डी से नुकसान

व्यस्क सुण्डी
कददूवर्गीय सब्जियों के लघुपद कीट
1. सफेद मक्खी:
वैज्ञानिक नाम: बैमेसीया टेबेसाई, कुल: एल्यूरोडिडी , गण: हेमिप्टेरा
पौषक पौधे: इस कीट के मुख्य पौषक पौधे कपास, तंबाकू, टमाटर और कददूवर्गीय सब्जियों आदि है.
आर्थिक क्षति एवं नुकसान: सफेद मक्खी की प्रकोप पत्तियों के निचली सतह पर सिराओं के बीच में होता है और यह पत्तिंयो से रस चूसती है. इस कीट का शुष्क मौसम के दौरान प्रकोप अधिक होता है और गतिविधि बारिश की शुरुआत के साथ घटती जाती है. इसके प्रभाव से पौधे की पत्तियां पीली पड जाती हैं, पत्ते सिकुड्ने और नीचे की ओर मुड जाते हैं. सफेद मक्खी वायरस रोग का संचारण करती है.
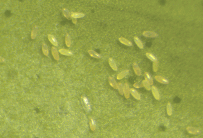
सफेद मक्खी के अण्डे

सफेद मक्खी के निम्फ

व्यस्क सफेद मक्खी
2. लीफ माइनर:
वैज्ञानिक नाम: लिरीयोमाइजा ट्राईफोलाइ , कुल: कुल: एग्रोमाइजीडी , गण: डिप्टेरा
पौषक पौधे: इस कीडे का आक्रमण सभी कद्दू कुल के पौधो मे होता है जैसे लौकी, करेला, तोरई, कद्दू, ककडी, खरबूजा, खीरा, टिंडा आदि.
आर्थिक क्षति एवं नुकसान: यह पत्तियों के ऊपरी भाग पर टेढे मेढे भूरे रंग की सुरंग बना देता है ओर इसका मेगट ही पत्तियों को नुकसान पहुचाता है.

मेगट से नुकसान

व्यस्क लीफ माइनर
3. चेपा:
वैज्ञानिक नाम: एफीस गोसीपी , कुल: एफीडिडी , गण: हेमिप्टेरा
पौषक पौधे: इस कीट के मुख्य पौषक पौधे कपास, तंबाकू, टमाटर और कददूवर्गीय सब्जियां है.
आर्थिक क्षति एवं नुकसान: इसके निम्फ व व्यस्क दोनों पत्तियों को नुकसान पहुचाते है. ये छोटे आकार के काले एवं हरे रंग के होते हैं तथा कोमल पत्तियों, पुष्पकलिकों का रस चूसते हैं.
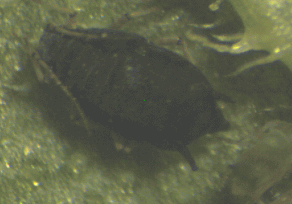
व्यस्क चेपा

निम्फ व व्यस्क से नुकसान
कददूवर्गीय सब्जियों में समेकित कीट प्रबन्धन:
सब्जियों में आईपीएम का महत्व ओर बढ़ जाता है क्योंकि फल और सब्जी मनुष्य द्वारा खाई जाती है। जो कीटनाशक ज्यादा ज़हरीले होते हैं या अपने ज़हरीले असर के लिए जाने जाते हैं उनकी सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। किसान ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कीटनाशकों के असर को खत्म होने के लिय समय नहीं देते और जल्द ही फसल को बाजार में बेच देते हैं। इस वजह से कीटनाशकों का ज़हर उनमें बाकी रह जाता है, कभी कभी इस वजह से मौत तक हो जाती है। इसलिए सब्जियों में कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। समेकित कीट प्रबंधन (आई. पी. एम.) का उपयोग फलों में 1940 के बाद किया गया. इससे पहले 1800 से 1940 तक कीट प्रबंधन के लिए तेल, साबुन, रेजिंस, पौधों से प्राप्त जहरीले पदार्थ एवं अकार्बनिक योगिकों का उपयोग होता था. 1940 के बाद सिंथेटिक व्यापक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा और इनका बार- बार अनुप्रयोग होने से कीटों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित होने लगी. इस प्रकार कीटों मे प्रतिरोधकता होने से ज्यादा कीटनाशकों का अनुप्रयोग होने लगा, जिससे वातावरण खराब होने लगा और कीटों के प्राकृतिक शत्रु नष्ट होने लगे. इन सब घटकों से बचाने के लिय समेकित कीट प्रबंधन (आई. पी. एम.) की कददूवर्गीय सब्जियों में आवश्यकता पडी.
समेकित कीट प्रबंधन (आई. पी. एम.) क्या है:
यह कीट प्रबंधन की वह विधी है जिसमें कि सम्बधित पर्यावरण तथा विभिन्न कीट प्रजातियों के जीवन चक्र को संज्ञान में रखते हुए सभी उपयुक्त तकनीकों एवं उपायों का समन्वित उपयोग किया जाता है, ताकि हानिकारक कीटों का स्तर आर्थिक नुकसान के स्तर के नीचे बना रहे.
आई. पी. एम. के उद्देश्य:
— न्यूनतम लागत के साथ-साथ अधिकतम फसल उत्पादन.
— मिट्टी, पानी व वायु में कीटनाशकों की वजह से न्यूनतम प्रदूषण.
— पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना.
इस प्रबंधन के अंदर निम्नलिखित घटक आते है: फल को पेपर या प्लास्टिक से ढकना, खेत की सफाई करना, प्रोटीन बैट और क्यू-आकर्षण ट्रैप, कीट प्रतिरोधक पौधे, जैविक नियंत्रण और कम विषैले कीटनाशकों आदि का उपयोग कीट को नुकसन के आर्थिक स्थर से नीचे रखने के लिये किया जाता है.
1. फल को पैपर या प्लास्टिक से ढकना:
पौधे के फलो को 2-3 दिन के अंतराल पर दो परत पैपर या प्लास्टिक से बांधना चाहिय जिससे की फल मक्खी अपने अण्डे फलों पर नहीं दे पाती है. इस प्रबंधन से 40-58% तक फलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है. इस प्रबंधन का उपयोग कददूवर्गीय फसलों जैसे तरबूज, खरबुज, ककडी, लौकी, तोरई, कददू आदि मे किया जाता है.
2. खेत की सफाई करना:
कीटों के प्रबंधन में सबसे प्रभावी तरीका खेत की सफाई करना होता है. फल मक्खी, चितकबरी सुंडी, लाल कद्दू बीटल, हाडा बीटल आदि के प्रजनन चक्र और जनसंख्या वृद्धि को तोड़ने के लिये गर्मी के दिनो मे खैत की गहरी जुताई करनी चाहिये. पौधों और फलों के क्षतिग्रस्त भागों को हटा देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए.
3. क्यू-आकर्षण ट्रैप:
क्यू-आकर्षण ट्रैप फल मक्खी के प्रबंधन मे प्रभाशाली है. क्यू-आकर्षण ट्रैप नर को आकर्षित करती है और इसके अंदर कीटनाशक रखा जाता है जिसके द्वारा नर मर जाता है और मादा संमभोग करने के लिये नर नहीं मिलता है. इस प्रकार से इन कीडों का प्रबंधन कर सकते है.
विभिन्न प्रकार के क्यू-लुर: 1) फलाईसीड ® 20%, ऊगेलुर ® 8%, क्यू-लुर 85%+ नैल्ड, क्यू-लुर 85%+ डाय्जिनोन, क्यू-लुर 95%+ नैल्ड आदि बाजार मे उपलब्ध हैं और इनको फल मक्खी को नियंत्रित करने में प्रभावी पाया गया है. 2) खेत में रात के समय प्रकाश के ट्रैप लगायें तथा उनके नीचे किसी बर्तन में चिपकने वाला पदार्थ जैसे सीरा अथवा गुड का घोल भर कर रखे।
4. जैविक नियंत्रण:
कीटों का नियंत्रण जैविक तरीको से करने का तरीका है ओर आईपीएम का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है. व्यापक अर्थ में, बायोकंट्रोल का अर्थ है जीवित जीवों का प्रयोग कर फसलों को कीटों से नुकसान होने से बचाना. कुछ बायोकंट्रोल एंजेट्स इस प्रकार हैं.
पैरासिटॉइड्स: ये ऐसे जीव हैं जो अपने अंडे उनके पोषक किटों के शरीर में या उनके ऊपर देते हैं और पोषक कीट के शरीर में ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं. परिणामस्वरूप, पोषक कीट की मृत्यु हो जाती है. एक पैरासिटॉइड्स दूसरे प्रकार का हो सकता है, यह पोषक कीट के विकास चक्र पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर वह अपना जीवन चक्र पूरा करता है. उदाहरण के लिए, अंडा, लार्वा, प्यूपा, अंडों के लार्वल और लार्वल प्यूपल पैरासिटॉइड्स निम्नलिखित है ट्राइकोगर्मा, अपेंटेलिस, ब्रैकोन, चिलोनस, ब्रैकिमेरिया आदि की विभिन्न प्रजातियां हैं.
प्रीडेटर्स: ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं. उदाहरण: मकड़ियां, ड्रेगन फ्लाई, मक्खियां, डेमसेल फ्लाई, लेडी बर्ड, भृंग, क्रायसोपा, पक्षी आदि प्रजातियां महत्वपूर्ण है.
5. कीट प्रतिरोधक पौधे लगाना:
कीट प्रतिरोधक पौधे समन्वित कीट प्रबंधन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटक है. यह किसी भी प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव से पैदा नहीं होता है और किसानों को कोई अतिरिक्त लागत भी नहीं आती है. अधिक उपज देने वाले पौधों और कीट प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए.
| सं | कददूवर्गीय सब्जियां | फल मक्खी प्रतिरोधी किस्में |
| 1. | करेला | आई एच आर-89 व आई एच आर-213 |
| 2. | घीया (लौकी) | एन बी-29, एन बी-22, एन बी-28 |
| 3. | कददू | आई एच आर-35, आई एच आर-40, आई एच आर 83 |
| 4. | तोरई | एन आर-2, एन आर-5, एन आर-7 |
| 5. | टिण्डा | अर्का टिण्डा |
| 6. | कद्दू | अर्का सूर्यमुखी |
रासायनिक नियंत्रण:
जब कीड़ों को समाप्त करने के सारे उपाय खत्म हो जाते हैं तो रासायनिक कीटनांशक ही अंतिम उपाय नजर आता है. कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकतानुसार, सावधानी से और आर्थिक नुकसान का स्तर (ईटीएल) के मुताबिक होना चाहिए. इस प्रकार न सिर्फ कीमत में कमी आती है बल्कि अन्य समस्याएं भी कम होती है. जब रासायनिक नियंत्रण की बात आती है तो किसानों को निम्न बातों का ध्यान रखते हुए अच्छी तरह पता होना चाहिए कि किस रासायनिक कीटनांशक का छिड़काव करना है, कितना छिड़काव करना है और कैसे छिड़काव करना है.
– ईटीएल और कीट प्रतिरक्षक अनुपात का ध्यान रखना चाहिए.
– सुरक्षित कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए, उदाहरण के तौर पर नीम आधारित और जैवकीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए.
– अगर कीट कुछ भागों में ही मौजूद हैं तो सारे खेत में छिड़काव नहीं करना चाहिए.
कददूवर्गीय सब्जियों के लिय निम्नलिखित रासायनिक कीटनांशक काम मे लेना चाहिए.
1. तने, पत्ती, फलों एवं फूल भेदकों के लिये रासायनिक कीटनाशी:
| रासायनिक कीटनाशी | रासायनिक कीटनाशी की मात्रा |
| डाइमीथोएट 30 ई सी | 1.5 से 2.0 मिली/ लीटर पानी |
| मैलाथियान 50 ई सी | 1.5 से 2.0 मिली/ लीटर पानी |
| स्पाईनोसेड 45 एस सी | 0.5 से 0.7 मिली/ लीटर पानी |
| इंडोक्सिकर्ब 14.5 एस सी | 0.5 से 0.7 मिली/ लीटर पानी |
2. तने, पत्ती, फलों एवं फूल चूसकों के लिये रासायनिक कीटनाशी
| रासायनिक कीटनाशी | रासायनिक कीटनाशी की मात्रा |
| प्रोफेनोफोस 50 ई सी | 1.5 से 2.0 मिली/ लीटर पानी |
| एसीफेट 75 एस पी | 1.5 से 2.0 मिली/ लीटर पानी |
| ईमीडाक्लोपरीड 17.8 एस एल | 0.5 से 0.7 मिली/ लीटर पानी |
| एसीटमेपरीड 20 एस पी | 0.5 से 0.7 मिली/ लीटर पानी |
| थायोमिथोक्ज़ाम 70 ड्ब्लू एस | 0.5 से 0.7 मिली/ लीटर पानी |
Authors:
Shravan M Haldhar (Scientist), B.R.Choudhary (Scientist) & Suresh Kumar (Research Associate)
CIAH, Bikaner (ICAR), Rajasthan
Mobile: 09530218711
Email: haldhar80@gmail.com



