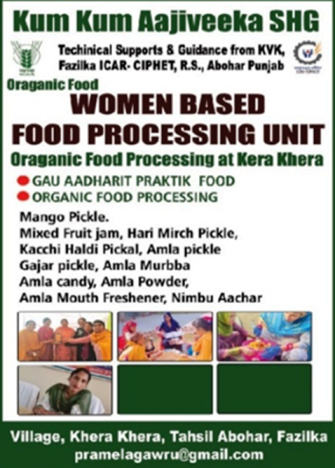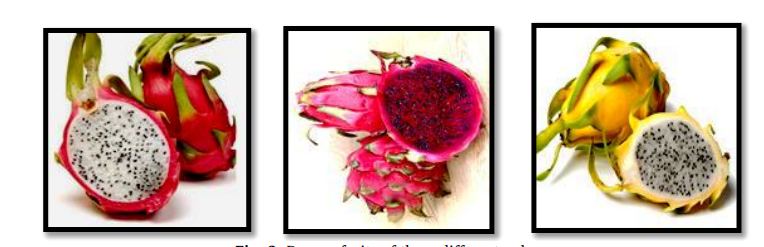20 Oct पपीते की खेती की समीक्षा और रोग प्रबंधन
Papaya cultivation Review and Diseases Management
पपीता एक उष्णकटिबंधीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया है। इसकी उत्पत्ति का स्थान कोस्टा रिका और दक्षिण मैक्सिको माना जाता है। यह एक सदाबहार फलदार वृक्ष है। पपीता बहुत ही पौष्टिक व स्वादिष्ट होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। यह विटामिन सी का अच्छा स्त्रोत है। इसके लाभदायक गुणों को देखते हुए ये हमारे दैनिक आहार का हिस्सा बन गया है।
पपीता की खेती भारत के अलावा ब्राजील, अमेरिका, मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, चीन, इथोपिया और थाईलैंड में भी बड़े पैमाने पर की जाती है।
भारतीय परिदृश्य
पुर्तगालियों द्वारा यह फल वृक्ष 1611 में भारत में लाया गया । भारत में पपीता का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं। भारत में पपीता उत्पादक क्षेत्र में 63 प्रतिशत वृद्धि जो कि 45.2 हजार हेक्टेयर 1991-92 में तथा 73.7 हजार हेक्टेयर 2001-2002 में दर्ज की गई है।
अब यह क्षेत्र 97.7 हजार हेक्टेयर हो गया है और सालाना पैदावार 3628.9 हजार मैट्रिक टन दर्ज की गई है। इसकी खेती अन्य फलदायक वृक्षों जैसे कि आम, अमरूद, बेर तथा नींबू के बीच खाली जगह में भी की जा सकती है। उत्तरी राज्यों में यह फसल डेढ़ साल बाद तथा दक्षिणी राज्यों में एक साल बाद फल देने लग जाती है।
पपीता की खेतीः
इसकी खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। रेतीली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। जिन क्षेत्रों में पाला पड़ता है और जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था नही है वहाँ पपीता की खेती नही की जा सकती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच अच्छा माना जाता है। पपीता का प्रवर्धन बीज के द्वारा किया जाता है। 300 ग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिये उपयुक्त होता है। पहले अप्रैल माह में क्यारियों में बीज डाला जाता है तथा जून माह तक खेत में रोपण के लिए पौध तैयार हो जाती हैं।
1.5 से 2 मीटर की दूरी पर 50×50 x 50 सै.मी. के गड्ढे खोदें तथा गड्ढों को खाद व मिट्टी की बराबर मात्रा डाल के भर दें। जूून माह के अलावा सितम्बर या अक्तूबर माह में भी पौधों का खेत में रोपण किया जा सकता है। इसके अलावा 25×10 सै.मी. आकार के पाॅलीथीन लिफाफों में भी पौध तैयार की जा सकती हैं। हर लिफाफे को रेत व गोबर खाद की बराबर मात्रा से भर के 2-3 बीज बोएं। सर्दी के दिनों में जहां अधिक ठंड हो व पाला पडता हो वहाँ नवम्बर से फरवरी माह तक पौधांे को घास-फूस या पाॅलीथीन से ढकें व समय समय पर सिंचाई करना उचित हैं।
पपीते में प्रायः नर एवं मादा दोनों पौधे पाये जाते हैं। जब फूल आने शुरू हो जाएं तब नर पौधों को निकाल देना चाहिए। पूरे खेत में अलग-अलग जगह पर केवल 10 प्रतिशत नर पौधे परागण की प्रक्रिया के लिये पर्याप्त होते है। पौधे को रोपण के बाद हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के दिनों में 7-8 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 12-14 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। पानी खड़े होने से किये जाने वाले नुकसान से बचने के लिए पौधे के चारों तरफ मिट्टी चढाना लाभदायक होता है। 20 किलोग्राम गोबर खाद प्रति पौधे के हिसाब से अवश्य दें।
इसके अलावा अधिक पैदावार के लिए प्रति पौधा आधा किलोग्राम मिश्रित खाद जिसमें अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट व पौटाशियम सल्फेट 2ः4ः1 के अनुपात में मिला हो, साल में दो बार (फरवरी व अगस्त माह) खाद डालें।
जब फल के रंग में परिवर्तन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि फल पक गया है। फलों को तोड़कर अलग-अलग कागज में लपेटकर, लकड़ी के बक्से या फाइबर के गत्ते में रख देना चाहिए। पपीता के पौधे की औसत उम्र 5 से 6 वर्ष तक ही होती है क्योंकि इसके बाद पैदावार घट जाती है। पपीता की प्रमुख किस्में पूसा डिलीशियस, पूसा ड्वार्फ, रेड लेडी 786, कुर्ग हनी, वाशिंगटन तथा हनीह्यु आदि हैं।
प्रमुख रोग एवं उपचारः-
आद्रगलन/ पपीता का डैंपिंग आफः
बहुत सी फफंूद जैसे कि पिथियम अफानिडर्मेटम, पिथियम अल्टीमम, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका और राइजेक्टोनिया मिल के यह रोग करते है। ये फफंूद नये अंकुरित पौधों को प्रभावित करता है और पौधे का तना जमीन के पास से सड़ जाता है और मर जाता है। इस रोग से बचाने के लिए बीज को थाइरम या केप्टान से 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। पौधशाला में बोर्डो मिश्रण (5ः5ः50) या मेनेकोजेब (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव 3 से 4 बार 7 दिन के अन्तराल पर करना लाभदायक है।
कली या पुष्प का सड़ना/ रोटिंग आफ पपाया (फाइटोप्थोरा पालमिवोरा):
इस फफूंद के प्रकोप से फल व कलिका के पास का तना पीला पड़ जाता है। फल पे अधिक प्रकोप होने के कारण फल सिकुड़ जाते हैं तथा अपरिपक्व अवस्था में ही झड़ जाते है। इसके नियंत्रण के लिये बोर्डो मिश्रण (5ः5ः50) का 2.5 प्रतिशत या काॅपर आक्सीक्लोराइड का 30 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए।
तना गलन या काॅलर राॅट (पिथियम अफानिडर्मेटम)
उपरोक्त फफूंद के अलावा फ्यूजेरियम और राइजेक्टोनिया भी इस रोग को बढावा देते हैं। ज्यादातर यह रोग अधिक नमी वाले इलाकों में पाया जाता है। इस रोग से पौधों को बचाने के लिए जल निकासी का उचित प्रबन्धन होना चाहिए। रोग का अधिक प्रकोप होने पे पत्तियां पीली पड़ जाती है व पौधों की बढवार भी प्रभावित होती है। अन्ततः पौधा सूख जाता है व फलों का आकार भी छोटा रह जाता है। इस बीमारी से बचाने के लिए पौधों के चारों ओर जल भराव को नही होने देना चाहिए। रोगग्रस्त पौधों को दिखते ही नष्ट कर देना चाहिए।
एन्थ्रेक्नोज/ फलों का सड़ना (कालेटोट्रिकम ग्लोइयोसप्रोइडेस):
यह रोग फल लगने से लेकर पकने तक किसी भी अवस्था में प्रभावित कर सकता है। शुरू में जलीय धब्बे दिखाई देते हैं जो कि बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। ये धब्बे फल की उपरी सतह से अंदर की तरफ धंसे हुए दिखाई देते है। इस रोग से फलों को बचाने के लिए केप्टान या डाइथेन एम-45 के 0.2 प्रतिथत घोल का छिड़काव 15 दिनों के अन्तराल में किया जाना चाहिए। इसके अलावा 0.2 प्रतिशत जीरम का उपयोग भी कर सकते है। सड़े हुए फलों को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए।
रिंग स्पाट (पपाया रिंग स्पाट विषाणु):
इस रोग में फल और तनों पर छोटे गोलाकार हरे पीले धब्बे बन जाते है। पत्तियां कटी-फटी हो जाती है तथा तैलिय व जलीय धब्बे भी दिखाई देते हैं। पौधे की पैदावार व फल की गुणवत्ता भी घट जाती है। यह रोग सफेद मक्खी एवं माहू से फैलता है। पौधों का रोपण बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए। कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 ई.सी. 2 मि.ली. प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना उचित है।
मौजेक (पपाया मौजेक विषाणु):
इस रोग के कारण पत्तियां छोटी हो जाती हैं। इस रोग में पत्ती के सम्पूर्ण पीले-हरे पटल पर फफोले होते हैं जो हरे उत्तकों को ढक लेते हैं। इस को मौजेक पैटरन बोल सकते हैं। यह रोग सफेद मक्खी एवं चेपा द्वारा फैलता है। इस रोग से ग्रस्त पौधों को तुरंत निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। सफेद मक्खी एवं चेपा की रोकथाम के लिए मैलाथियान 50 ई.सी. (0.1 प्रतिशत) 250 मि.ली. दवा का 250 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव उचित है।
पत्ती मोडन/ लीफ कर्ल (पपाया लीफ कर्ल विषाणु):
रोग ग्रस्त पपीते के पौधे की पत्तियां मुड़ी हुई तथा शिराएं पीली पड़ जाती है। पत्तियाँ आकार में सामान्य पत्तियांे से छोटी रह जाती हैं तथा छूने पर मोटी व भुरभरी लगती है। फलों का आकार छोटा हो जाता है तथा पैदावार बहुत कम हो जाती है। रोगग्रस्त पौधों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। पपीते के खेत के नजदीक कपास व भिण्डी नही लगानी चाहिए। समय समय पर कीटनाशक जैसे कि मैलाथियान 50 ई.सी. का छिड़काव करके पौधों को इस रोग के प्रकोप से बचाया जा सकता है।
Authors
प्रोमिल कपूर* एवं लोकेश यादव
*सहायक वैज्ञानिक (पादप रोग विभाग),
पादप रोग विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
Corresponding Author – kapoorpromil@gmail.com