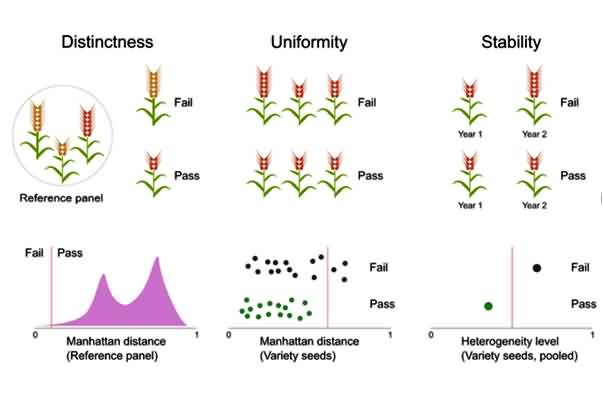16 Dec Durum wheat: characteristics, products and improved varieties
कठिया (डयूरम) गेहूँ की विशेषताएं, उत्पाद एवं उन्नतशील प्रजातियाँ
भारत के लगभग सभी प्रान्तों मे गेहूँ की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। भारत मे खेती करने के लिए मुख्य रूप मे दो तरह के गेहूँ प्रचलित है एक साधारण गेहूँ जिसको एस्टीवम कहते है और दूसरा कठिया गेहूँ जिसे डयूरम कहते है। गेहूँ के कुल उत्पादन में सामान्य गेहूँ (एस्टीवम) 95 प्रतिशत, एवं कठिया गेहूँ (डयूरम) का लगभग 4 प्रतिशत योगदान है।
कठिया गेहूँ ट्रिटिकम परिवार मे दूसरे स्तर का महत्वपूर्ण गेहूँ है। गेहूँ के तीनो उप-परिवारो (एस्टीवम, डयूरम, डायकोकम) मे उत्पादन की दृष्टि से डयूरम का दूसरा स्थान है। भारतवर्ष मे कठिया गेहूँ की खेती लगभग 25 लाख हैक्टर में की जाती है। इसकी खेती मध्य भारत के मालवांचल, गुजरात का सौराष्ट्र और कठियावाड, राजस्थान का कोटा, मालावाड तथा उदयपुर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड मे की जाती है।
ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नही है के लिए कठिया गेहूँ एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योकि इसमे सामान्य गेहूँ के मुकाबले सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है।
कठिया गेहूँ के पौधे, सामान्य गेहूँ के मुकाबले मोटे होते है एवं इसकी पतियों भी चौडी होती है। इसके दाने अधिक कठोर, बडे आकार के, सुनहरी रंग के तथा अर्द्धपारदर्शी होते है। इसके अलावा कठिया गेहूँ मे ग्लूटन प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है और इसीलिए कठिया गेहूँ अपने विशेष गुणों एवं विभिन्न प्रकार के उत्पादों में प्रयुक्त होने के कारण वर्तमान समय में अधिक महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए प्रयोग मे लाया जाता है।
कठिया गेहूँ की सबसे बडी खासियत यह है कि इसमें सामान्य गेहूँ के मुकाबले अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसमे बीटा कैरोटीन नामक एक पीला पदार्थ पाया जाता है। जिससे शरीर में विटामिन ‘‘ए‘‘ बनता है जोकि सामान्य गेहूँ मे बिल्कुल भी नही पाया जाता है। यह पीला पदार्थ आँखो की बिमारियों के लिए बहुत फायदेमंद होता हैं।
वैसे तो भारतवर्ष मे प्राचीन काल से ही कठिया गेहूँ की खेती की जाती रही है। परन्तु वर्तमान समय मे कठिया गेहूँ की खेती का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढता ही जा रहा है इसका प्रमुख कारण, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे इसकी बढती मांग को माना जा रहा हैं। जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कठिया गेहूँ की कीमत, सामान्य गेहूँ के मुकाबले 20 प्रतिशत तक अधिक होती है।
कठिया गेहूँ प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित लघु उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योकि इससे बनने वाले सिमोलिना (सूजी, रबा) से विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे पिज्जा, पास्ता, नूडल एवं सिवैय्या आदि तैयार किये जाते है।
शीघ्र पचनीय पौष्टिक आहार मे कठिया गेहूँ बहुत अच्छा माना जाता है। इससे बनने वाला दलिया एवं रोटी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। तथा मधुमेह (शुगर) रोगियो के लिए कठिया गेहूँ का आहार बहुत फायेदेमंद माना जाता है।
कठिया गेहूँ की विशेषताएं
कठिया गेहूँ में विटामिन बी कॉम्पलेक्स जैसे कि थाइमीन एवं फोलेट प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है जोकि हमारी आँखो, बालो, त्वचा, लीवर को स्वस्थ रखने मे मदद करता है। इसके अलावा यह हमारी तंत्रिका प्रणाली एवं दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। कठिया गेहूँ मे विटामिन बी, फाइबर, आहार, मिनरल, विटामिन ई प्रचुर मात्रा मे एवं कोलेस्ट्रोल बहुत ही कम मात्रा मे पाया जाता है। अतः कठिया गेहूँ को प्रतिदिन के पुष्ट आहार मे भी सम्मिलित किया जा सकता है। कठिया गेहूँ मे निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है।
- कठिया गेहूँ मे लौहा एवं सेलेनियम प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है। लौहा हमारे शरीर मे खून की कोशिकाओ के प्रसार एवं पुर्ननिर्माण मे मदद करता है। जबकि सेलेनियम एक प्रतिउपचायक (एंटीऑक्सिडेंट) के रूप मे कार्य करता है। जोकि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है।
- कठिया गेहूँ मे बीटा कैरोटीन नामक पीला पदार्थ पाया जाता है जिससे विटामिन ‘‘ए‘‘ बनता है जोकि हमारी आखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है।
- कठिया गेहूँ की ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामान्य गेहूँ की तुलना मे अधिक होती है। जिसके कारण, इससे मिलने वाली कार्बोहाइड्रेट को शर्करा मे बदलने मे ज्यादा समय लगता है। अतः जिन व्यक्तियों को शुगर की बीमारी होती है। उनके रक्त मे शुगर का स्तर नही बढता जिसके कारण रक्त मे शुगर की मात्रा नियत्रित रहती है।
- कठिया गेहूँ मे आवश्यक खनिज जैसे मैग्नीषियम व कैल्शियम पाये जाते है। जोकि हमारे शरीर मे हडि्डयो का मजबूती प्रदान करने मे मदद करते है।
- सेमोलीना जोकि कठिया गेहूँ के अन्तबीजो (भ्रूणपोश) से बनाया जाता है जिसमे लोहे की मात्रा पाई जाती है लौहा हमारे शरीर मे हिमोग्लोबिन (रूधिर वर्णिका) के निर्माण मे अहम् भूमिका निभाता है और शरीर मे खून की कमी को पूरा करने मे मद्द करता है।
- कठिया गेहूँ में सोडियम व पौटाशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है। जोकि हमारे वृक्को (गुर्दो) को स्वस्प रखने के लिए बहुत आवश्यक है।
- कठिया गेहूँ में पौटाशियम प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है जोकि हमारे दिल की धडकन को सामान्य रखने मे मदद करता हैं। वही सोडियम व पौटाशियम की संतुलित मात्रा हमारे वृक्को (गुर्दो) मे होने वाली क्रोनिक (चरकरी) की बीमारी से बचाता है।
- कठिया गेहूँ में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन तथा खनिज अधिक मात्रा मे होने के कारण पौष्टिकता के आधार पर कठिया गेहूँ, सामान्य गेहूँ से अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ पास्ता एवं मेकोरोनी जैसे खाद्य उत्पादो मे प्रयोग होने के कारण विश्व बाजार मे कठिया गेहूँ की बहुत मांग है। जिसके कारण भारत का किसान इसकी खेती करके अतिरिक्त लाभ ले सकता हैं और भारत कठिया गेहूँ के उत्पादन एवं निर्यात मे विश्व मे अग्रणी देश बन सकता है।
कठिया गेहूँ से बनने वाले उत्पाद
सेमोलीना
कठिया गेहूँ के अर्न्तबीज (भ्रूणपोश) की पिसाई करके बनाये गये आटे को सेमोलीना कहते है। सेमोलीना मे ग्लूटन प्रोटीन की मात्रा अधिकता मे पाई जाती है। कई प्रकार के पकवान बनाने के लिए कठिया गेहूँ से बना सेमोलीना का प्रयोग किया जाता है।
अच्छी तरह तला हुआ सेमोलीना डफ (मुशाबक), परिपक्व सेमोलीना डफ (हरीकेल) और परिपक्व, सुजी, वनस्पति घी, चीनी और बादाम (हलवा) आदि का प्रचलन भी कई देश मे है। भारत में कठिया गेहूँ को पास्ता गेहूँ एवं मेकोरानी गेहूँ भी कहा जाता है क्योकि मोटे दानो की पिसाई करके सेमोलीना बनाया जाता है और इसी सेमोलीना से पास्ता, नूडल्स, एवं मेकोरानी आदि उत्पाद बनाये जाते है।
पास्ता
कठिया गेहूँ का प्रयोग पास्ता बनाने मे कच्चे माल के रूप मे किया जाता है और यही पास्ता अपने प्रमुख गुणो के कारण जैसे व्यापक विविधता के प्रकार, लम्बा अचल जीवन, अच्छी पौशण कीमत, आरोग्य सम्बन्धी गुणवत्ता एवं कम कीमत की वजह से वैश्विक स्तर पर खाने के रूप मे बहुत अधिक पसंद किया जाता है।
पास्ता बाजार मे विभिन्न रूपो मे उपलब्ध है। जैसे मेकोरानी (खाली टयूब) स्पीगिति (भरमा डंडी), नूडल्स (चपती/अण्डाकार) ट्रिप वर्तमान मे जैसे- जैसे लोगो मे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढी है एवं लोगो के पास विभिन्न कारणो से भोजन बनाने का समय घटता जा है। वैसे-वैसे कठिया गेहूँ के पास्ता उत्पादो की खपत दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है।
पास्ता वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से खाया जाने वाला उत्पाद है जोकि दानेदार सुजी को पानी मे मिलाकर बनाया जाता है एवं एक अच्छी गुणवत्ता का पास्ता बनाने के लिए कठिया गेहूँ मे ग्लूटन प्रोटीन की सबलता पर निर्भर करता है। पीला रंग (पिगमेंट) की उपलब्धता, एवं उच्च प्रोटीन की उपलब्धता, एक उच्च गुणवत्ता का पास्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
कठिया गेहूँ मे कैरोटिनायड की अधिकता होने के कारण, इसके बनने वाले पास्ता मे पीला रंग की अधिकता होती है। अतः इससे बनाये गये पास्ते की बनावट अधिक संघन एवं दृढ तथा अधिक लोचदार होती है।
पास्ता, मानव षरीर मे ग्लुकोज की मात्रा को कम करने मे मदद करता है जिसके कारण यह मधुमेह की बीमारी से बचाने मे मददगार साबित होता है। पास्ता मे वसा एवं सोडियम की मात्रा का स्तर कम या अधिक होने के कारण इसकी प्रतिदिन के स्वास्थ्य आहार मे सम्मिलित किया जा सकता है।
कसकस
कसकस एक पास्ता उत्पाद है जोकि सेमोलीना को पानी के साथ मिलाने से बनता है। एक अच्छा कसकस बनाने के लिए कठोर दाने एवं सेमोलीना का रंग, मन का आधार, प्रोटीन की मात्रा तथा ग्लूटन प्रोटीन की सबलता महत्वपूर्ण होती है। अधिक प्रोटीन एवं सबलता ग्लूटन से कसकस का उत्पादन व गुणवत्ता दोनो बंढते है कसकस शाकाहारी प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत माना जाता है जोकि हृदय रोग एवं कैंसर जैसी घातक बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है।
बुलगर
बुलगर, कठिया गेहूँ को उबालकर बनाया जाने वाला एक बहुत ही पुराना उत्पाद है। कठिया गेहूँ के दाने मे अधिक कठोरता एवं दानो का रंग सुनहरा होने के कारण, सामान्य गेहूँ के मुकाबले कठिया गेहूँ को अधिक पसंद किया जाता है। मोटे बुलगर को चावल की तरह उबालकर खाया जाता है तथा बारीक बुलगर को मीट के साथ मिलाकर पकाया जाता है। बुलगर को तुर्की, सीरिया, जोर्डन, लेबनान, तथा मिश्र मे मुख्य दावत के रूप में प्रयोग किया जाता है।
फ्रेकह
फ्रेकह बिना पकी हरी गेहूँ को सुखाकर बनाया जाता है फ्रेकह को खाने हेतू पकाने के लिए पानी मे डालकर 20 मिनट तक गर्म करके तथा 5 मिनट तक ठण्डा करते है। फ्रेकह को चावल, बुलगर एवं कसकस की तरह ही प्रयोग किया जाता है। फ्रेकह उत्तरी अफ्रीका एवं मध्य-पूर्व विषेष रूप से सीरिया मे भोजन के रूप मे प्रचलित है और इसको चावल की तरह ही पकाकर भोजन के रूप मे खाया जाता है।
कठिया गेहूँ की उन्नतशील किस्में
| डीडीडब्ल्यू 47: यह किस्म भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा विकसित की गई है सिंमित सिचाई वाले क्षेत्रों मे समय से बुवाई करने पर इसकी औसत उपज 37.3 कु. प्रति है. पाई जाती है इस किस्म मे पीला रंजक तत्व की अधिकता है। |  |
| डीडीडब्ल्यू 48: यह किस्म सिंचित क्षेत्रों मे समय से बुवाई करने पर 47.4 कु. प्रति है. की औसत उपज देती है। इसके दानो मे प्रोटीन व पीला रंजक की अधिकता होती है एवं यह किस्म काला व भूरा रतुआ प्रतिरोधी है। |  |
| एचआई 8777 (पूसा गेहूँ 8777): यह किस्म भारतीय गेहूँ कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, इंदोर द्वारा विकसित की गई है। समय से बिजाई करने पर इसकी औसत उपज 18.5 कुन्तल प्रति हैक्टर पाई गई है। इसकी खेती प्रायद्वीपीय क्षेत्र के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों मे की जाती है यह किस्म भूरा रतुआ के प्रति प्रतिरोधक भी पाई गई एवं इसके दानो मे 14.3 प्रतिशत प्रोटीन, 43.6 पीपीएम जस्ता एवं 48.7 पीपीएम लौहा भी पाया जाता है। |  |
| एचआई 8737 (पूसा अनमोल): यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर द्वारा मध्य क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। सिंचित क्षेत्रो मे समय से बुवाई करने पर 53.4 कु. प्रति है की औसत उपज देती है। इस किस्म मे पीला व भूरा रतुआ के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है एवं इसमे पीला रंजक तत्व 5.38 पीपीएम 12.1 प्रतिषत प्रोटीन भी अधिकता मे पाया जाता है। |  |
| एचआई 8713 (पूसा मंगल): यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर द्वारा मध्य क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। सिंचित क्षेत्रो मे समय से बुवाई करने पर इसकी औसत उपज 52.3 कु. प्रति है. पाई जाती है यह किस्म काला व भूरा रतुआ के लिए प्रतिरोधी है। एवं इसमे पीला रंजक तत्व 7.16 पीपीएम भी पाया जाता है। |  |
| एचआई 8805: यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर द्वारा सिमित सिंचाई वाले क्षेत्रां के लिए विकसित की गई है। समय से बुवाई करने पर 23.4 कु. प्रति है. की औसत उपज देती है। इसके दानो मे 12.8 प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है एवं यह किस्म काला रतुआ प्रतिरोधी किस्म है। |  |
| एचआई 8802: यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, इन्दौर द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों मे समय से बिजाई करने पर 36 कु. प्रति है. की औसत उपज देती है। इसके दानां मे 13.0 प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। यह किस्म काला रतुआ प्रतिरोधी है। |  |
| एचडी 8759 (पूसा तेजस): यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन, इंदोर द्वारा मध्य क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। सिंचित क्षेत्रों मे समय से बिजाई करने पर इसकी औसत उपज 56.9 कुन्तल प्रति हैक्टर पाई गई है। इसके दानों मे लौहा एवं जस्ता की अधिकता पाई जाती है। एवं यह किस्म पास्ता बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके दानो मे 12.0 प्रतिशत प्रोटीन, 42.8 पीपीएम जस्ता एवं 42.1 पीपीएम लौहा भी पाया जाता है। |  |
| एचडी 4728: यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा मध्य क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। यह किस्म सिंचित क्षेत्रो मे समय से बुवाई करने पर 54.2 कुन्तल प्रति हैक्टर की औसत उपज देती है। यह किस्म काला व भूरा रतुआ प्रतिरोधी है। इसका दाना मोटा व शोभायमान होता है। |  |
| जीडब्ल्यू 1346: यह किस्म कृषि अनुसंधान केन्द्र, धदुका, ए.ए.यू. आनंद द्वारा विकसित की गई है सिमित सिंचाई क्षेत्रों मे समय से बुवाई करने पर 40.4 कु. प्रति है. की औसत उपज देती है। इसके दानो मे 12.36 प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। यह किस्म भूरा व काला रतुआ प्रतिरोधी है। |  |
| एमएसीएस 4028: यह किस्म आगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। समय से बुवाई करने पर उसकी औसत उपज 19.3 कुन्तल प्रति हैक्टर पाई गई है। यह किस्म भूरा रतुआ के प्रति प्रतिरोधक है। एवं इसके दानों मे 14.7 प्रतिशत प्रोटीन 40.3 पीपीएम जस्ता एवं 46.1 पीपीएम लौहा पाया जाता है। |  |
| एमएसीएस 3949: यह किस्म आधरकर अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रां के लिए विकसित की गई है। समय से बुवाई करने पर इसकी औसत ऊपज 44 कुन्तल प्रति हैक्टर पाई गई है। यह किस्म भूरा रतुआ के प्रति प्रतिरोधी है इसके दाने मे 12.9 प्रतिशत प्रोटीन, 0.6 पीपीएम जस्ता एवं 38.6 पीपीएम लौहा पाया जाता है। यह किस्म पास्ता बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। |  |
| एनआईडीडब्ल्यू 1149: यह किस्म कृषि अनुसंधान केन्द्र, निफाड द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों मे समय से बुवाई करने पर 29.4 कु. प्रति है. की औसत उपज देती है यह किस्म काला व भूरा रतुआ प्रतिरोधी है। |  |
| पीडीडब्ल्यू 291: यह किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा उतर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। सिंचित क्षेत्रों मे समय से बुवाई करने पर इसकी औसत उपज 47.6 कु. प्रति है. पाई जाती है। इसमें पीला व भूरा रतुआ, करनाल बंट फ्लैग स्मट के प्रतिरोधिता पाई जाती है। |  |
| डब्ल्यूएचडी 948: यह किस्म चौधरी चरण सिहं कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र (महाराष्ट्र व कर्नाटक) के लिए विकसित की गई है। सिंचित क्षेत्रो मे समय से बुवाई करने पर इसकी औसत उपज 46.5 कुन्तल प्रति हैक्टर पाई गई है। इसमे काला व भूरा रतुआ के प्रति प्रतिरोधता पाई जाती है इसके दाने मे 12.7 प्रतिशत प्रोटीन, 5.99 प्रतिशत पीला पदार्थ, पाया जाता है। तथा यह किस्म पास्ता बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। |  |
| डब्ल्यूएचडी 943: यह किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा उत्तर पष्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। सिंचित क्षेत्रों मे समय से बुवाई करने पर इसकी औसत उपज 48 कु. प्रति है. पाई गई है। इस किस्म में करनाल बंट के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। |  |
| यूएएस 415: यह किस्म कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए विकसित की गई एक प्रमुख किस्म है। सिंचित क्षेत्रों में समय से बुवाई करने पर इसकी औसत ऊपज 50 कुन्तल प्रति हैक्टर पाई गई है। यह किस्म भूरा व काला रतुआ, पर्ण झुलसा एवं चूर्णिल आसिता के प्रति प्रतिरोधक पाई जाती है। इसके दानों में 11.4 प्रतिशत प्रोटीन, व 4.49 पीपीएम पीला पदार्थ पाया जाता है। |  |
| यूएस 428: यह किस्म, कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रां के लिए विकसित की गई है। समय से बुवाई करने पर इसकी औसत उपज 47.9 कुन्तल प्रति हैक्टर पाई गई है। इस किस्म मे पीला व भूरा रतुआ एवं पर्ण झुलसा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है। इसके दाने मे 12.4 प्रतिशत प्रोटीन, 38.2 पीपीएम लौह, 30.4 प्रतिशत पीपीएम जस्ता एवं 5.49 प्रतिशत पीला पदार्थ भी पाया जाता है। |  |
| यूएएस 446: यह किस्म कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड, द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। वर्षा आधारित क्षेत्रों मे समय से बिजाई करने पर इसकी औसत ऊपज 18.3 कु. प्रति है. पाई गई है। इसके दानो मे प्रोटीन 13.9 प्रतिशत एवं पीपीएम 5.7 प्रतिशत पीला पदार्थ भी पाया जाता इसमे काला व भूरा रतुआ प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। |  |
| यूएएस 466: यह किस्म कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड द्वारा विकसित की गई है। सीमित सिंचाई क्षेत्रों मे समय से बुवाई करने पर 38.8 कु. प्रति है. की औसत ऊपज देती है। इसके दानों मे 12.3 प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। यह किस्म काला व भूरा रतुआ प्रतिरोधी है। |  |
Authors
चरण सिंह, प्रदीप कुमार, विकास गुप्ता, उमेश कांबले, गोपाल रेड्डी के, चन्द्रनाथ मिश्र, संतोष कुमार बिश्नोई एवं रविन्द्र कुमार
भा.कृ.अनु.प. – भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001, हरियाणा
Email: n_charansingh@hotmail.com (Corresponding author)