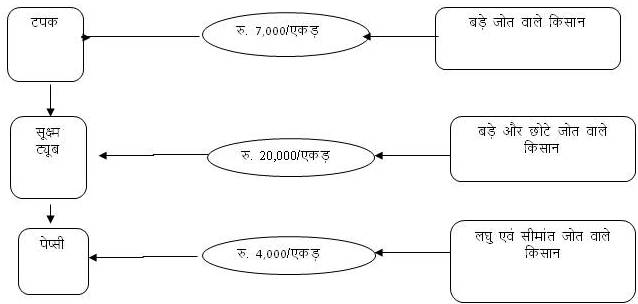23 Feb मृदा एवं जल संरक्षण में मेढ़ बंधीकरण (बंडिंग) का महत्व
Importance of Bounding in Soil and Water Conservation
मेढ़ बंधीकरण (बंडिंग) सीमांत, ढलान एवं पहाड़ी भूमि के लिए एक पारंपरिक, कम लागत वाला ,सरल भूमि प्रबंधन अभ्यास है । यह तकनीक मृदा – अपरदन को नियंत्रित करने, जल प्रतिधारण को बढ़ाने एवं फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु सफलतापूर्वक उपयोग की जाती है।
मेढ़ (बंड) एक मिट्टी की तटबंध है जिसे ढलान को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है, एवं ढलान की लंबाई को कम करके मृदा-अपरदन को कम किया जाता है। यह मृदा-अपरदन को नियंत्रित करने के लिए एक यांत्रिक / अभियांत्रिकीय विधि है।
इस अभियांत्रिकीय उपाय में मुख्य रूप से ढलान वाली भूमि सतह का संशोधन करके बहते हुए जल को संरक्षित किया जाता है एवं इस जल के बहाव से उत्पन्न होने वाले मृदा क्षरण/ कटाव में कमी आती है।
मेढ़ बंधीकरण के मुख्य उद्देश्य:
(i) यह भूमि सतह पर जल के ठहराव के समय को बढ़ाता है एवं भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है,
(ii) कई बिंदुओं पर बाधा उत्पन्न करके जलप्रवाह गति को कम करता है, एवं (iii) मिट्टी को जल के प्रवाह से होने वाले क्षरण से बचाता है।
मेड़ (बंड्स ) के प्रकार एवं उनको बनाने के तरीके
मेड़ एक तटबंध है जिसका निर्माण भूमि ढलान कि लंबवत दिशा में किया जाता है । खेतों में मृदा क्षरण नियंत्रण एवं नमी संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के बंड का उपयोग किया जाता है।
जब मेड़ों का निर्माण कंटूर (समान बिंदुओं को जोड़ने) वाली रेखाओं पर किया जाता है, तो उन्हें कंटूर (समोच्च) बंड के रूप में जाना जाता है। यदि कुछ ढलानों के साथ बंड का निर्माण किया जाता है, तो उन्हें ग्रेडेड (श्रेणीबद्ध) बंड के रूप में जाना जाता है।
बंडों पर कोई खेती नहीं की जाती है, परन्तु कुछ जगह बंड की सुरक्षा के लिए कुछ प्रकार के स्थिरीकरण घास लगाए जाते हैं। बंड के प्रकारों का चुनाव भूमि ढलान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार एवं खेतों में बंड निर्माण के उद्देश्य पर निर्भर करता है।
पारगम्य मिट्टी वाले कृषि क्षेत्र जिसकी वार्षिक वर्षा (<600 मिमी), एवं भूमि ढलान (<6% ) हो उन स्थानों पर कंटूर बंड का निर्माण किया जाता है, , जबकि ग्रेडेड बंड का निर्माण उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त जल बहाव के सुरक्षित निकास के लिए किया जाता है।
हमारे देश में कंटूर एवं ग्रेडेड मेड़ बंदीकरण का अभ्यास काफी प्रचलित है एवं हमारे किसान इससे भली-भांति परिचित हैं । भारत के कई हिस्सों खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में कंटूर बंडिंग का उपयोग बहुप्रचलित है। अनुभव से, यह पाया गया है कि बंड उथले, मध्यम एवं मध्यम गहरी मिट्टी में अच्छी पकड़ बनाये रखते हैं।
यद्यपि काली मिट्टी में विभिन्न क्षरण की समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की मिट्टी में समोच्च बंडिंग को सफलतापूर्वक उपयोग नहीं किया जा सकता है। । गहरी काली मिट्टी में, शुष्क स्थिति में दरारों के कारण, बंड विफल हो जाते हैं। इन दरारों के माध्यम से, पानी खेतों के अंदर बहता है और इसके परिणामस्वरूप फसलों को गंभीर नुकसान होता है।
 कंटूर या समोच्चच बंड
कंटूर या समोच्चच बंड
यह हमारे देश में सर्वाधिक प्रचिलित बंडिंग प्रणाली है। इन मेड़ों को मुख्यतः वर्षा आधारित फसलों वाले खेतों में निर्मित किया जाता है । कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुख आवश्यकता मिट्टी में फसल के उपयोग के लिए वर्षा जल का संरक्षण है एवं इसके लिए फील्ड स्ट्रिप को कोई अनुदैर्ध्य ढलान प्रदान नहीं किया जाता है।
बंडिंग की इस प्रणाली में, बंड को जहां भी आवश्यक हो, मामूली समायोजन कर कंटूर रेखाओ पर बनाया जाता है ।
संशोधित समोच्च बंडिंग में तटबंधों का निर्माण समोच्च रेखा पर किया जाता है एवं क्षेत्र के निचले सिरे पर गेटेड आउटलेट बनाया जाता है । यह गेट-आउटलेट वांछित अवधि के लिए क्षेत्र में रनऑफ को स्टोर करता है, और फिर स्पिल्वे के माध्यम से पूर्व निर्धारित दर से जल को निकासित करता है।
इस प्रकार यह बंड के पीछे जल के ठहराव के समय को कम करता है , जिससे फसल की वृद्धि और उपज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
इन बंड के टूटने कि संभावना बहुत कम होती है, जबकि पारम्परिक कंटूर बंडस में लम्बे समय तक जल के भराव के कारण इनके टूटने की संभावना बहुत अधिक रहती है।
गेट आउटलेट कंटूर बंड सिस्टम में एक निश्चित अवधि में जुताई और अन्य कृषि सम्बन्धी कार्य संभव है।
समोच्च बंड या कंटूर मेढ बंधीकरण की सीमाएं हैं:
- यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- यह चिकनी एवं काली मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है
- यह 6% से अधिक भूमि ढलानों पर उपयुक्त नहीं है।
 ग्रेडेड बंड या मेढ
ग्रेडेड बंड या मेढ
उच्च वर्षा वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ की भूमि मृदा अपरदन के प्रति अतिसंवेदनशील हो, मृदा कम पारगम्य हो एवं जलमग्नता (वॉटर लॉगिंग) की समस्या बनी रहती हो, में ग्रेडेड मेड बनायीं जाती है ।
इस प्रणाली का उपयोग अतिरिक्त जल-बहाव को सावधानीपूर्वक कृषि क्षेत्रो से बाहर निकालने में किया जाता है । इसे मुख्यतः आउटलेट की ओर अग्रसर अनुदैर्ध्य ढलान पर एक ढाल के रूप में बनाया जाता है । ढाल, एकसमान या परिवर्तनशील हो सकती है ।
एकसमान वाले ग्रेडेड बंड उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं जहाँ कम लंबाई के बंडों की आवश्यकता एवं जल का बहाव कम होता है ।
जबकि परिवर्तनशील ग्रेडेड बंड उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं जहाँ बंडों की लंबाई अधिक होती है एवं रनऑफ जल की मात्रा निकासी की तरफ बढ़ती जाती है ।
इस प्रकार की मेड़ो में, मेड के विभिन्न भागो में उसके ढाल में परिवर्तनशीलता प्रदान की जाती है ताकि जल प्रवाह की चाल वांछित सीमाओं के भीतर रहे जिसके कारण मृदा अपरदन न हो।
ग्रेडेड बंडिंग में बंड के ठीक ऊपरी हिस्से में जल निकास के लिए छोटी नालियां बनाई जाती हैं एवं इन नालियों से निकलने वाले जल को सुरक्षित आउटलेट आमतौर पर ग्रास्ड वॉटर वे (Grassed water-ways), के माध्यम से खेतों के बाहर निकला जाता है।
ग्रेडेड बंड नैरो- बेस या ब्रॉड – बेस हो सकते हैं। आमतौर पर इन बंड्स का निर्माण लगभग 2-10 प्रतिशत भूमि ढलान पर और उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 600 मिमी से अधिक होती है।
आमतौर पर भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रेडेड बंड की डिज़ाइन नैरो – बेस टैरेसिंग (terracing) के समान होती है।
ग्रेडेड बंड सिस्टम की सीमाएं हैं:
- ये बंड कृषि उपकरणों को पार करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- नियमित अंतराल पर उचित देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता होती है।
बंड के डिजाइन विशिष्टता
बंड डिज़ाइन के लिए निम्नलिखित पैरामीटर पर विचार किया जाना चाहिए:
बंड का प्रकार: बंड निर्माण करने के लिए (समोच्च या वर्गीकृत बंड) प्रकार, वर्षा और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। कंटूर बंड को 600 मिमी से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जाती है, जहां मिट्टी की नमी फसल उत्पादन के लिए एक सीमित कारक होती है। अधिक वर्षा के सुरक्षित निकासन के लिए एवं भारी और मध्यम वर्षा क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ग्रेडेड बंड बनाए जाते हैं । बंड का ग्रेड 0.2% से 0.3% तक हो सकता है।
बंडों के बीच का अंतराल:
बंडों के बीच का अंतराल निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करता है :
- ऊपरी बंड के नीचे सीपेज जोन (रिसाव क्षेत्र) को निचले बंड के सेचुरेशन जोन (संतृप्ति क्षेत्र) से मिलना चाहिए;
- बंडों को उन बिंदुओं पर जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करना चाहिए जहां जल तीव्र वेग प्राप्त करता है एवं
- बंड कृषि सम्बंधित कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए ।
बंड का आकार: बंड के आकार में इसकी ऊंचाई, ऊपरी चौड़ाई, साइड ढलान एवं नीचे की चौड़ाई शामिल है। बंड की ऊंचाई मुख्य रूप से भूमि की ढलान, बंडों के बीच की दूरी एवं क्षेत्र में संभव अधिकतम वर्षा पर निर्भर करती है। एक बार बंड की ऊंचाई निर्धारित हो जाने के बाद, बंड के अन्य आयामों जैसे आधार की चौड़ाई, ऊपरी चौड़ाई और साइड ढलान , वहाँ की मिट्टी के अनुसार निर्धारित की जाती है।
बंड का निर्माण
बंड का निर्माण ऊपरी भाग (रिज) से प्रारम्भ करके नीचे (वैली) की ओर करना चाहिए। यदि निर्माण के दौरान बारिश होती है तो यह तरीका बंडों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जिस जगह पर बंड का निर्माण करना हो उस स्थान को अच्छे से साफ़ किया जाना चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मिटटी कंकर-पत्थर, घांस तथा अन्य वनस्पति आदि रहित हो एवं मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए।
बंड बनाने हेतु मिट्टी के लिए गड्ढे आम तौर पर बंड के ऊपरी हिस्से में बनाए जाते हैं। गड्ढे नाली या निचले क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए। जब मिट्टी खोदी जाती है, तो ढेलों और पत्थरों को उसके साथ ही हटा दिया जाना चाहिए।
मिट्टी को 15 सेमी की परतों में रखा जाना चाहिए और फिर किसी भारी यंत्र के द्वारा इसको अच्छी तरह से दबाना चाहिए। बंड को अंत में वांछनीय आकार दिया जाना चाहिए, ऊपर और किनारों पर मिट्टी को सही तरीके से दबाकर थोड़ा सा घुमाव दिया जाना चाहिए।
बंड निर्माण के बाद, खेत और गड्ढे को हल चलाकर समतल किया जाना चाहिए। उचित देखभाल और रखरखाव के लिए, घांस व अन्य वनस्पतियों को बंड पर लगाना चाहिए।
बंड का उचित उपयोग
एक अनुमान के मुताबिक, भारत में बंडिंग के तहत कुल क्षेत्र लगभग 383.8 हेक्टेयर है, जिसका उपयोग फल – फूल या चारे के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक खाली भूमि का उचित उपयोग करेगी और साथ ही किसानों को पूरक आय प्रदान करेगी।
वर्षा निर्भर क्षेत्रों में नीम, खेजड़ी , कुमठ, करोंदा, सागौन आदि पेड़ों को लगाया जा सकता है जबकि सिंचित भूमि में आँवला, नीबू , अमरुद, जामुनसकती बांस आदि पेड़ों को लगाया जा सकता है । पशुओं हेतु चारा प्राप्ति के लिए बाजरा – नेपियर, अंजन, दशरथ, हाथी घाँस को लगाया जा सकता है ।
इस प्रकार डोली या बंड की उचित देखभाल और रखरखाव से मृदा व जल संरक्षण के साथ-साथ खाली भूमि से पूरक आय सुनिश्चित की जा सकती है।
“ हर खेत पर मेड़, हर मेड़ पर पेड़ ”
Authors:
अजिता गुप्ता1, अमित कुमार पाटील1, चेतनकुमार सावंत2
1वैज्ञानिक, आईसीएआर-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसन्धान, झाँसी (उ. प्र.)- 284 003
2वैज्ञानिक, आईसीएआर- केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संसथान, भोपाल (म. प्र.)– 462 038
Email: ajitagupta2012@gmail.com