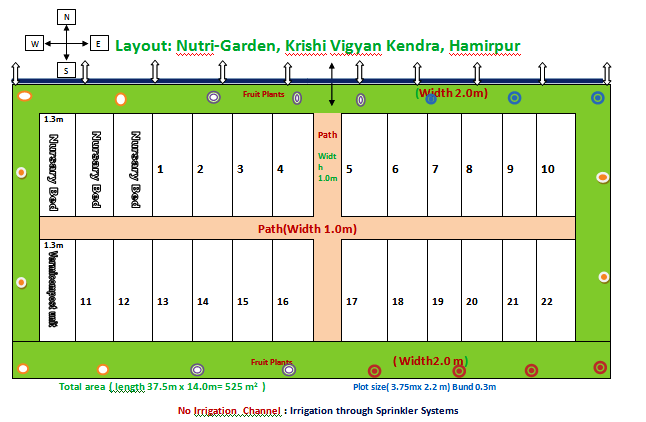25 Aug खरीफ सब्जी फसलों में होने वाले प्रमुख रोग एवं उनका प्रबन्धन
11 Major Diseases and their management in Kharif vegetables crops
सब्जियां उनकें पोषक तत्वों जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो अम्ल एवं खनिज पदार्थ आदि की धनी स्रोत होने के कारण मनुष्य के भोजन का आवश्यक अंग है।
इंडियन कॉन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद के द्वारा संस्तुत भारत में सब्जी की प्रति व्यक्ति मांग 300 ग्राम के विपरीत केवल 130 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्ध है।
हमारे देश में वैश्विक सब्जी उत्पादन का नेतृत्व करने की पर्याप्त क्षमता है किन्तु सब्जी अनेक रोग व्याधियों के प्रति संवेदनशील होने के कारण हमारा सब्जी उत्पादन एवं उत्पादकता कम हो जाता है।
भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब आदि में सामान्यतः किसान फसल चक्र के सिद्धान्तों का पालन नही करते है जिसके कारण रोगों को फलने-फूलने के लिए अनुकूल दशाऐं मिल जाती है परिणामस्वरूप फसलों में भारी क्षति होती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत लेख में खरीफ सब्जियों में होने वाले मुख्य रोगों की पहचान-निदान एवं प्रबन्धन प्रस्तुत किया गया है –
1. आर्द्रपतन रोग (डेम्पिंग ऑफ):
यह रोग खीरा, लौकी, काशीफल, आदि को प्रभावित करता है। यह रोग मृदा जनित है एवं पीथियमस्पेशीज, फाइटोफ्थोरा स्पेशीज एवं राइजोक्टोनिया स्पेशीज द्वारा होता है परन्तु पीथियम अफेनीडर्मेटम प्रमुख रोगकारक है।
रोग लक्षणः
आर्द्रपतन नई पौध या बीजांकुरों का सामान्य रोग है। यह उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहां पर नमी की अधिकता तथा खेतों में जल निकास का उचित साधन नही होता है। यह रोग लगभग सभी शाक सब्जियों को भारी क्षति पहुंचाता है।
यह रोग दो अवस्थाओं में आता है (अ) अंकुरण पूर्व (ब) अंकुरण पश्चात। अंकुरण पूर्व अवस्था में नये अंकुरित पौधें मृदा की सतह से बाहर निकलने से पहले ही मर जाते है।
बीज गल जाता है अथवा बीजांकुर नये मूलांकुर (रेडिकल) एवं प्रांकुर (प्लूमूल) की गलन के कारण मर जाते है। अंकुरण पश्चात अवस्था संक्रमित बीजांकुरो के भूमि से निकलने पर किसी भी समय भूमि पर धराशायी होने से पहचानी जाती है। रोगी बीजांकुर पीले हरे होते है एवं उन पर कॉलर क्षेत्र पर मृदा सतह के पास एक भूरा विक्षत या धब्बा पाया जाता है। संक्रमित उत्तक सड़ जाते है और बीजांकुर नष्ट होकर धराशायी हो जाते है।
रोग प्रबन्धनः
- नर्सरी के लिये उभरी हुई बीज शैय्या तैयार करनी चाहिये जिससे जल निकास आसानी से हो सके। नर्सरी की मृदा हल्की बलुई होनी चाहिए।
- बीजों को घना नही बोना चाहिये अर्थात पौधें से पौधें का उचित अन्तराल या दूरी रखें।
- उचित जल निकास के साथ फसल की आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिये।
- बुवाई से पहले कैप्टान अथवा थाइराम से 2.5-3.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करना चाहिये। बीज को ट्राइकोडर्माविरिडीकेकवक संवर्द्ध से 4 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने पर अंकुरण पूर्व आर्द्रपतन का प्रभावशाली नियन्त्रण हुआ है।
- फॉर्मेलीन डस्ट (15 भाग फॉर्मेलीन एवं 85 भाग चारकॉल राख) के द्वारा 30 ग्राम प्रति वर्ग फुट भूमि की दर से उपचार करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है।
- भारी संक्रमण होने पर मृदा की कैप्टान अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से 2.0 ग्राम प्रति लीटर जल की दर से ड्रेन्चिंग करनी चाहिये।
- मृदा का कवकनाशी रसायन (0.2 प्रतिशत कैप्टान या 0.2 प्रतिशत कॉपर सल्फेट या 0.2 प्रतिशत फॉर्मेलिन) से उपचार करना चाहिए। फॉर्मेलिन के प्रयोग के बाद बीज बुवाई से पहले रसायन की गन्ध निकल जानी चाहिये।
2. शुष्क म्लानि और जड़ गलनरोग (विल्ट व रूट रोट):
यह रोग लगभग सभी कद्दुवर्गीय फसलों को प्रभावित करता है। यह रोग मृदा जनित है एवं फ्यूजेरियम प्रजाति एवं वर्टिसिलियम प्रजाति के द्वारा होता है।
रोगलक्षणः
यह जमीन में उपस्थित कवक से फैलता है। इस रोग से फसल किसी भी अवस्था में ग्रसित हो सकती है।
रोग के प्रथम लक्षण शिराओं एवं सहायक शिराओं का सुस्पष्टन, पत्तियों की हरिमाहीनता एवं पर्ण वृन्तों का मुरझाकर झुकना अथवा क्लांतिनत होना है। शुरूआत में पौधें पीले दिखाई देते है।
परपोषी की जड़ो और स्तंभ का निचला भाग शुष्क विलगन से नष्ट हो जाता है। रोगग्रस्त भाग पर काले बिन्दु समान स्क्लेरोशियम मिलते है। यदि तने के आधार का छिलका हटाकर देखें तो उत्तक भूरे रंग के दिखते है।
यह भूरा रंग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। तरूण पौधें अकस्मात सूखकर नष्ट हो जाते है। जड़े काली पड़कर सड़ जाती है जिससे पौधा जल्दी सूखने लगता है। पौधों के अवशेष पर गुलाबी रंग का कवकजाल देखा जा सकता है।
नई छोटी पत्तियां एक के बाद एक करके मर सकती है और पूरा पौधा म्लानि होकर कुछ ही दिनों में मर सकता है। शीघ्र ही पर्णवृन्त एवं पत्तियां म्लानि होकर गिर जाती है। खेत में निचली पत्तियां पहले पीली पड़ जाती है और तब ग्रसित पत्रक मुरझाकर मर जाता है।
लक्षण बाद की पत्तियों पर भी जारी रहते हैं। बाद की अवस्था में संवहन तंत्र भूरा बादामी हो जाता है। पौधें बौने रह जाते है और अन्ततः मर जाते है।
रोग प्रबन्धनः
- खेत की सफाई रखें। रोगी पौधों को उखाड़कर जला दें।
- सब्जियों की रोग रोधी प्रजातियां उगाए।
- गैर परपोषी पौधों जैसे धान्य फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाए। फसल चक्र का प्रयोग करके इस रोग को काफी हद तक रोका जा सकता है।
- गर्मियों में गहरी जुताई करें।
- बीज को 0.3 प्रतिशत थायराम या कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किग्रा की दर से उपचारित करके बुवाई करना चाहिये।
- कार्बेन्डाजिम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर जल की दर से ड्रेन्चिंग करनी चाहिये।
- बरसात में फसल में जल निकास का उचित प्रबन्ध करना चाहिये।
- गर्मी की फसल को समय से सिंचाई करते रहना चाहिये।
3. जीवाणु जम्लानि रोग (बैक्टेरियल विल्ट):
कद्दुवर्गीय फसलों का यह रोग स्यूडोमोनाससोलेनेसियेरमनामक जीवाणु से होता है।
रोग लक्षणः
यह सब्जियों के सबसे गंभीर रोगों में से एक है। सापेक्षतः अधिक मृदा नमी एवं मृदा तापमान रोग के विकास के लिए अनुकूल होते है। जीवाणुज म्लानि के विशिष्ट लक्षण बौनापन, पीलापन एवं पर्ण समूह का मुरझाना एवं उसके बाद पूरे पौधें का नष्ट होना है।
निचली पत्तियां म्लानि से पहले क्लांतिनत हो जाती है। रोगजनक अधिकांशतः संवहन तंत्र क्षेत्र तक सीमित होता है परन्तु रोग की अग्रिम अवस्था में यह वल्कुट (कॉर्टेक्स) एवं मज्जा (पिथ) क्षेत्र में आक्रमण कर सकता है और उत्तको का पीला-भूरा विवर्णन कर देता है।
रोग ग्रसित पौधों का भाग जब काटकर पानी में डुबोया जाता है तो कटे हुऐ भाग से जीवाणुज निपंक (बैक्टेरियल ऊज) की स्पष्ट श्वेत वर्णरेखा दिखाई देती है। पत्तियां पीली नही होती और उन पर या फलों पर किसी प्रकार के धब्बें नही बनते है। अधिकतर आक्रांत पौधें अकस्मात मुरझाकर झुक जाते है। यह मृदोढ़ रोग है।
रोग प्रबन्धनः
- गैर परपोषी पौधों जैसे धान्य फसलों के साथ फसल चक्र अपनाने से सब्जियों में जीवाणुज म्लानि का रोग प्रसार घटता है।
- जीवाणुग्रस्त खेतों का बीज प्रयोग न करें।
- यह रोग पौधों में घावों, भूमि अथवा कृषि यन्त्रों के द्वारा फैलता है। फसलों में घाव न लगने दें। खेत में ब्लीचिंग पावडर का 10 किग्रा प्रति हैक्टेअर की दर से प्रयोग करें।
4. फल विगलन रोग (फ्रूटरोट):
यह कवक जनित रोग है जो करेला, लौकी, खीरा, सीताफल, तरबूज आदि अन्य कुकरबिट्स फसल को प्रभावित करता है। यह रोग पिथीयम,फाइटोफ्थोरा, फ्यूजेरियम,क्लेडोस्पोरियम, स्केलेरोशियमआदि कवको की प्रजातियों के द्वारा होता है।
रोगलक्षणः
फलों पर रोग का प्रारम्भ पीताम्भ-भूरे, संकेन्द्री वलय युक्त धब्बों के रूप में होता है। यें धब्बें आकार में छोटे हो सकते है या फल का अधिकांश भाग आच्छादित कर सकते है। छिलके का विलगन नही होता लेकिन फल के भीतरी केन्द्र तक गूदा बदरंग हो सकता है। कभी-कभी फल पर रूई के समान कवक की वृद्धि आ जाती है जो पूरे फल को ढ़क सकती है। यह प्रायः पिथीयमके कारण होती है। छोटे एवं हरे फल संक्रमण होने पर सिकुड़ जाते है। अधिकतर पके फल बाद में जीवाणु जनित मृदु विलगन से नष्ट हो जाते है। पर्ण अंगमारी भी हो सकती है। कभी-कभी फलों पर धब्बों में संकेन्द्री वलय नही पाए जाते हैं।
रोगप्रबन्धनः
- फसल चक्र अपनाए।
- खरपतवारों को नष्ट कर दें।
- रोगी फलों को तोड़कर नष्ट कर दें।
- पानी की अच्छी निकासी करें।
- डाएथेन एम-45 या जिनेब (1.5 किलोग्राम प्रति 500 लीटर पानी/हैक्टेअर) का छिड़काव।
5. मृदुरोमिल आसिता रोग (डाउनी मिल्ड्यू):
यह रोग लौकी,खीरा, तरबूज, खरबूजा आदि फसलों में नुकसान करता है। यह रोग स्यूडोपेरोनोस्पोराक्यूबेन्सिस,पेरोनोस्पोराप्रजाति के द्वारा होता है।
रोग लक्षणः
रोग संक्रमण पौधें के विकास के किसी भी अवस्था में हो सकता है। रोग लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर बिखरें हुए पीले से भूरे अनेक प्रकार की आकृति के धब्बों के रूप में दिखाई देते है।
बीज शैय्या में बीजपत्रक व प्राथमिक पत्तियां पहले ग्रसित होती है जिसके कारण पत्ती की निचली सतह पर कवक की वृद्धि दिखलाई पड़ती है। बाद में इस वृद्धि के विपरीत पत्ती की ऊपरी सतह पर हल्का पीलापन बन जाता है।
नयी पत्ती अथवा बीजपत्रक पीले पड़ने के बाद गिर जाते है। पुरानी पत्तियां सामान्यतः थमी रहती है और संक्रमित भाग धीरे-धीरे चमकीला और पीला-भूरा व कागज के समान हो जाता है।
कभी-कभार रोग ग्रसित पत्ती पर सैकड़ों सूक्ष्म गहरे बिन्दू बन जाते है। ठण्ड़ी और नम दशाओं में रोग ग्रसित पत्ती की निचली सतह पर बनें विक्षत पर एक सफेद मृदुरोमिल आसिता वृद्धि दिखाई देती है।
रोग प्रबन्धनः
- स्वच्छ खेती जैसे स्वच्छ बीज शैय्या का प्रयोग़ और रोग ग्रसित फसल अवशेष और खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिये।
- साफ एवं रोग रहित बीज ही बोना चाहिये।
- 2-3 वर्ष का फसल चक्र अपनाया जाए तो भूमि में पड़े निषिक्तांड़ निष्क्रिय हो जाते है।
- ऐसे स्थान एवं ऐसे पौध अन्तरण का प्रयोग करें जिससे पौधों पर सूर्य का प्रकाश पूरे दिन पड़ता रहे।
- यदि गम्भीर रोग दबाव सम्भावित हो तो फसल पर डाएथेन एम-45 अथवा डाएथेन जेड-78 का 1.0-1.2 किग्रा प्रति हैक्टेअर की दर से छिड़काव करना चाहिये।
6. चूर्णिल आसिता रोग (पाउडरी मिलड्यू):
यह रोग कुकरबिटेसी कुल की फसलों को प्रभावित करता है। यह रोग ऐरीसाइफीप्रजातिकवक के द्वारा होता है।
रोग लक्षणः
सर्वप्रथम रोग पौधें की पत्तियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधें के दूसरे भाग पर भी फैल जाता है। आरम्भ में पत्तियों की दोनों सतह पर सफेद चूर्णी धब्बें बनते है, जो बाद में फल एवं तने इत्यादि के ऊपर भी बन जाते है जिससे पूरा पौधा मुरझा जाता है।
पत्तियां गंभीर संक्रमण में सिकुड़कर सूख जाती है। शीघ्र ही इन चूर्णी धब्बों का रंग भूरा हो जाता है। पहले धब्बें छोटी- छोटी रंगहीन चित्तियों के रूप में बनते है, परन्तु अन्त में इनके चारों ओर चूर्णी समूह फैल जाता है।
रोग की गम्भीर अवस्था में सम्पूर्ण पौधें की सतह सफेद चूर्ण जैसे पदार्थ से ढ़क जाती है। यह पृष्ठीय चूर्ण समूह वास्तव में परजीवी का कवकजाल एवं बीजाणु होते है। रोगी पौधों में वाष्पोत्सर्जन एवं श्वसन क्रियायें बढ़ जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है।
इस प्रकार से रोगी पौधें छोटे रह जाते है और उन पर फल भी कम लगते है तथा भार में हल्के होते है। पत्तियों के जिस स्थान पर परजीवी का कवकजाल फैला रहता है, वहां की कोशिकयें उत्तकक्षय के कारण मर जाती है। यह सूखे मौसम व कम तापमान होने पर काफी तेजी से फैलता है।
रोग प्रबन्धनः
- भूमि में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को एकत्र करके जला देना चाहिये।
- खेत के आसपास कवक की उत्तरजीविता के स्रोत तथा खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिये।
- क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत फसल की रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करनी चाहिये।
- 25 से 30 किलोग्राम प्रति हैक्टेअर की दर से गन्धक चूर्ण (300 मेश) को बुरकना चाहिये।
- किसी घुलनशील गन्धकयुक्त कवकनाशी रसायन जैसे थायोविट या सल्फेक्स का 1.0 से 1.2 किग्रा प्रति हैक्टेअर अथवा कैराथेन या कैलेक्सीन का 1.0 से 1.2 लीटर प्रति हैक्टेअर का 10 से 15 दिन के अन्तराल पर दो से तीन बार छिड़काव करें।
- रोग से रक्षा हेतू टेबूकोनाजोल का 500 ग्राम प्रति हैक्टेअर 12-15 दिनों के अन्तराल पर छिड़कना चाहिये। रोग का घनत्व अधिक होने पर यह अन्तराल घटाया जा सकता है।
7. चार कोल विलगन रोग (चारकोलरोट):
यह कुकरबिटेसी कुल की सब्जियों का प्रमुख रोग है। यह मैक्रोफोमिना फैजियोलिना फफूंद के द्वारा होता है।
रोग लक्षणः
यह कद्दुवर्गीय फलों की प्रमुख समस्या है। भारत में जहां भी कद्दुवर्गीय फसल उगायी जाती है वहां पर यह रोग पाया जाता है। रोग के शुरूआती लक्षण फलों पर थोड़े से धंसे हुये गुलाबी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई पडते है।
फलों पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बें बनते है जो अनुकूल वातावरण मे तेजी से बढ़ते है। जैसे-जैसे रोग बढ़ता है पूरा फल रोग ग्रसित हो जाता है। फल की सतह स्कलेरोशिया के कारण काली हो जाती है। फल का गूद्दा काला हो जाता है और उसमें स्कलेरोशिया भर जाते है।
रोग के अधिक गंभीर होने पर फल का गूद्दा चारकोल पाउडर में बदल जाता है। बीज राख जैसे धूसर रंग के हो जाते है। इस रोग द्वारा ग्रसित पौधों के पर्ण समूह गर्म मौसम में म्लानि व पीलापन दर्शाते हैं।
रोग प्रबन्धनः
- शीघ्र पकने वाली किस्में लगायें।
- प्रभावित फल व पौधें के अन्य भाग तोड़कर नष्ट कर दें।
- साफ एवं रोग रहित बीज ही बोना चाहिये।
- बीज को बोने से पूर्व बाविस्टीन (0.2 प्रतिशत) अथवा विटावैक्स (0.2 प्रतिशत) से उपचारित करें।
8. डाई बैक अथवा श्याम व्रण एवं फल विगलन रोग (एन्थ्रेक्नोज व फ्रूट रोट):
यह रोग कुकरबिटेसी कुल की सब्जियों को प्रमुखतः प्रभावित करता है। यह रोग कोलेटोट्राइकम प्रजाति के द्वारा होता है।
रोग लक्षणः
फल गलनः इस रोग में केवल परिपक्व फल प्रभावित होते है। फल की त्वचा पर एक छोटा गोलाकार काला धब्बा प्रकट होता है और यह लम्बे ध्रुव की दिशा में फैलता है और इसलिए यह कम या ज्यादा दीर्घवृत्तीय या दीर्घवृतक हो जाता है।
जैसे यह संक्रमण बढ़ता है यह धब्बें मिलकर रंग में काले अथवा हरे अथवा मैले धूसर अथवा यें स्पष्टत रूप से मोटे और नुकीले काले बाह्यरेखा से हल्के काले या तिनके जैसे भूरे पीले रंग के क्षेत्र को घेरे हुए सीमांकित होते है।
बुरी तरह प्रभावित फल सामान्य रंग के बदले तिनके जैसे भूरे पीले रंग के हो जाते है। इस विवर्णन क्षेत्र पर कवक की असंख्य बिखरी हुई एसरवुलाई पायी जा सकती है।
जब रोगी फल को काटा जाता है तो फल की निचली सतह पर कवक सूक्ष्म बारीक, उभरी हुई गोलाकार काली स्ट्रोमैटिक समूह अथवा स्केलेरोशिया दिखाई देती है।
रोग की अग्रिम अवस्था में बीज कवक के कवकजाल से ढ़क जाता है। ऐसे बीजों का रंग जंग जैसा दिखाई देता है।
डाई बैकः विकसित पौधों में रोग के कारण शाखाओं का कोमल शीर्ष उत्तकक्षयी होकर सूख जाता है। यह सूखना फिर नीचे की ओर बढ़ता है। इस अवस्था को शीर्षारंभीक्षय (ड़ाईबैक) कहते है।
सम्पूर्ण शाखा अथवा पौधें का सम्पूर्ण शीर्ष मुरझा जाता है। मृत शाखाएं जलासिक्त से भूरी हो जाती है और रोग की अग्रिम अवस्था में धूसर सफेद से तिनके जैसे पीले रंग की हो जाती है।
प्रभावित शाखाओं की उत्तकक्षयी सतह पर बहुत सी बिखरी हुई काले बिन्दु (एसरवुलाई) बन जाती है। कभी-कभी उत्तकक्षयी क्षेत्र स्वस्थ क्षेत्र से एक गहरी भूरी से काली पट्टी द्वारा अलग होता है।
केवल शीर्ष अथवा कुछ बगल की शाखाएं अन्ततः मर जाती है अथवा सम्पूर्ण पौधा मुरझा जाता है। आंशिक रूप से ग्रसित पौधें पर कुछ निम्न गुणवत्ता वाले फल लगते है।
रोग नियन्त्रणः
- बीज को स्वस्थ धब्बें विहीन फलों से एकत्र करना चाहिये।
- साफ एवं स्वस्थ बीज का थाइराम अथवा बाविस्टीन से 2.0-2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से उपचार करना चाहिये।
- कवकनाशी रसायन जैसे ब्लाइटॉक्स-50 अथवा फाइटोलॉन अथवा डाईथेन एम-45 (1.0-1.2 किग्रा प्रति हैक्टेअर की दर से 500 लीटर पानी) का छिड़काव रोग दिखाई देने के बाद 10-15 दिन के अन्तराल पर करें।
- रोगी पौधों एवं खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिये।
- रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग सबसे प्रभावशाली नियन्त्रण विधि है।
9. पत्तियों का चितकबरा रोग (मौजेक रोग):
यह रोग खीरा, करेला, लौकी, सीताफल आदि को प्रभावित करता है। यह विषाणु जनित रोग है।
रोग लक्षणः
इस रोग का विशिष्ट लक्षण पत्तियों का चितकबरा होना है। यह चितकबरापन अनियमित आकार के हल्के हरे या पीले धब्बों और पत्ती के सामान्य हरे धब्बों की उपस्थिति के रूप में प्रकट होता है। यें धब्बें धंसे या उभरे हुए हो सकते है।
पत्तियों के किनारे नीचे झुक जाते है और कड़े हो जाते है। पत्तियों के आकार में भारी कमी आ जाती है और वें धागें नुमा दिखाई देती है। संक्रमित पौधों पर फूलों व फलों की संख्या में कमी आ जाती है। फल विकृत एवं खुरदरें हो जाते है।
गंभीर रूप से संक्रमित पौधें बौने रह जाते है और वे अधिक संख्या में विकृत व मांसल पत्तियों के साथ झाड़ीनुमा दिखाई देते है। यह विषाणु माइजसपर्सिकी नामक माहू व अन्य रस चूसने वाले कीटों से संचारित होता है।
रोग प्रबन्धनः
- स्वस्थ बीज ही प्रयोग करें।
- रोगी पौधों के अवशेषों एवं जंगली खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिये।
- रोगग्रस्त पौधों उखाड़कर सावधानीपूर्वक जला देना चाहिये व इन हाथों से स्वस्थ पौधों का स्पर्श न करें।
- डायमेथोयेट-30 ईसी का 150 ग्राम प्रति हैक्टेअर अथवा इमिडाक्लोप्रिड-17.8 का 125 मिलीलीटर प्रति एकड़ का रोपाई के 21 दिन बाद से 15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव माहू व अन्य रस चूसने वाले कीटों का अच्छा निंयत्रण करता है।
10. पर्ण कुंचन रोग (लीफ कर्ल):
यह विषाणु जनित रोग है जो कद्दुवर्गीय फसलों आदि को ग्रसित करता है।
रोग लक्षणः
पर्ण कुंचन रोग हमारे देश में अनेक सब्जी फसलों की गंभीर समस्या बनकर उभरा है। इस रोग के विशिष्ट लक्षण पत्तियां छोटी, नीचे और ऊपर की ओर मुड़ी हुई तथा एक जगह एकत्रित दिखलाई पड़ती है। पर्णक विकृत हो जाते है।
पत्तियां खुरदरी तथा मोटी हो जाती है। कुछ दशाओं में शिरा उदभासन (वेन क्लीयरिंग) भी पाया जाता है। पत्तियों के आकार में भारी कमी आ जाती है। पौधें बौने हो जाते है व पौधें का रूप झाड़ी समान हो जाता है। आक्रांत पौधों का रंग पीला हो जाता है।
उग्र आक्रमण में फूल नही बनते हैं। यह विषाणु स्वस्थ पौधों में बेमिसियाटेबैकी नामक सफेद मक्खी से संचारित होता है।
रोग प्रबन्धनः
- संक्रमित पौधों और खरपतवार को उखाड़ कर जला देना चाहिये।
- रोग वाहक कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करें।
- पौध के अच्छे से चलने पर ऐसिटामिप्रिड-20 घुलनशील चूर्ण का 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 15 दिनों के अन्तराल पर दो बार और प्रयोग करने पर रोग वाहक कीट का सर्वोत्तम नियन्त्रण करता है।
11. आल्टर्नेरिया पत्ती धब्बा रोग (आल्टर्नेरिया लीफ स्पॉट):
यह लौकी, खीरा, तोरई व अन्य कुकरबिट्स फसलों पर होता है। यह रोग कवक जनित है। जो आल्टर्नेरियाकुकुमेरिना एवं आल्टर्नेरिया आल्टर्नेटा फफूंद के द्वारा होता है।
रोग लक्षणः
यह रोग पत्तियों की उपरी सतह पर छोटे गहरे भूरे रंग़ के धब्बों के रूप में बनता है। यें धब्बें गम्भीर होने पर मिलकर बडे विक्षत बनाते है।
इन धब्बों में संकेन्द्री कटक द्वारा लक्ष्यपट्ट प्रभाव (टारगेट बोर्ड) भी दिखाई दे सकता है। यह रोग गर्म एवं आर्द्र मौसम में अधिक बढता है।
रोग प्रबन्धनः
- रोग रहित स्वस्थ बीज का प्रयोग करें।
- फसल पर डाएथेन एम-45 अथवा डाइफॉल्टान-80 घुलनशील चूर्ण अथवा डाएथेन जेड-78 का 1.0-1.2 किलोग्राम प्रति हैक्टेअर अथवा फाइटोलान का 1.2-1.5 किलोग्राम प्रति हैक्टेअर की दर से छिड़काव करने पर रोग का प्रभावी नियन्त्रण होता है।
- प्रतिरोधी किस्म बोने के लिये प्रयोग करें।
Authors:
*रविन्द्र कुमार, अनुजा गुप्ता एवं वी. के. महेश्वरी
*Scientist (Plant Pathology)
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय स्टेशन,करनाल-132001, हरियाणा
Email: ravindrakumarbhu@gmail.com