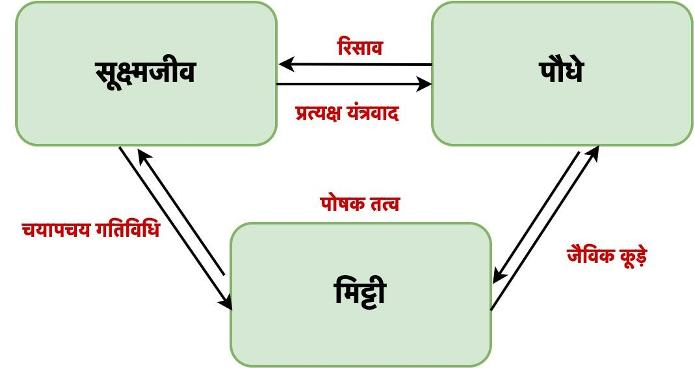15 Sep मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं मृदा परीक्षण की अनिवार्यता
Necessity of soil health card and soil testing
कृषि उत्पादकता बढाने के लिए मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान केंदित करना अत्यंत आवश्यक है इस बात को ध्यान मे रखते हुऐ वर्तमान सरकार ने पूरे देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है। इसमे मृदा का परीक्षण करना तथा उसका ब्योरा रखना बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड की विशेषताएं
-
सरकार ने इस योजना के तहत पुरे भारत के 14 करोड़ से भी ज्यादा किसानों तक इस स्कीम से जोडने की सोचा है।
-
यह योजना भारत के हर क्षेत्र में उपलब्ध है।
-
इस योजना से जुड़े हुए सभी किसानों को उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऑनलाइन और प्रिंट कर के दिया जाता है। मिटटी के परिक्षण के बाद इसमें उनके खेत की मिटटी के विषय में सभी जानकारियाँ दी जाती है।
-
हर किसान को उनके मृदा का स्वास्थ्य कार्ड प्रति 3 वर्ष में दिया जाता है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या-क्या जानकरी लिखा होता है?
-
किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा सैंपल नंबर होता है।
-
मृदा का स्वास्थ्य की यह मिटटी फसल करने के लिए सही है या नहीं।
-
मिटटी की विशेषताएं और सामान्य सिफारिशें।
-
मिटटी में उपलब्ध सभी पोषक तत्व।
-
मिटटी में किन-किन खाद का किन-किन अनाज के फसल में कितना उपयोग करना चाहिए उसकी जानकरी।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के फायदे
-
इस स्कीम की मदद से किसानों को अपने खेत की मिटटी के बारे में सही स्वास्थ्य जानकारी मिल पायेगी। इससे वो मन चाहे अनाज या फसल ले सकते हैं।
-
मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर 3 साल में सरकार प्रदान करती है जिसके कारण किसान को अपने मिटटी के बदलाव के बारे में भी बीच-बीच में पता चलते रहेगा।
-
इस योजना के तहत किसानो को अच्छी फसल उगाने में मदद मिलेगी जिससे उन्हें और देश दोनों का फायदा होगा।
-
इससे किसानों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश उन्नति की और बढेगा।
मिट्टी की जॉच
-
मिट्टी जॉच से मतलब है किसी खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का सही मूल्यांकन करना।
-
भूमि के स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए निरंतर अच्छी पैदावार पाने के लिए मिट्टी जाँच के आधार पर उर्वरकों व आवश्यक भूमि सुधार रसायनों का अनुशंसित मात्रा में इस्तेमाल करना आवश्यक है।
-
मिट्टी जॉच से हमें आमतौर पर यह मालूम होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जस्ता इत्यादि की कितनी मात्रा मौजूद है, मिट्टी की बनावट कैसी हैं या कोई अन्य समस्या तो नही है।
-
जॉच से यह भी पता चलता है कि मिट्टी फसल के लिए उपयुक्त है या नहीं, तथा उसमें कौन-कौन सी और कितनी खाद डालनी है।
मिट्टी का नमूना लेने की विधि
भारत सरकार द्वारा इस योजना में मिट्टी का नमूना लेना हेतु निम्नानुसार प्रामर्श निर्धारित किये है।
-
सिंचित क्षेत्रों में – प्रत्येक 2.5 है. इकाई क्षेत्र में एक नमूना ।
-
असिंचित क्षेत्रों में – प्रत्येक 10 है. क्षेत्र में एक नमूना।
- आधे किलोग्राम के एक नमूने को पूरे आधे हेक्टेयर या एक एकड़ के लगभग दस लाख किलोग्राम मिट्टी का प्रतिनिधित्व करना है।
- नमूना लेने का समय
-
अपने फार्म के प्रत्येक खेत कीे मिट्टी की अलग-अलग जॉच करवाये और कम से कम तीन वर्ष में एक बार जाँच अवश्य कराएं।
-
जॉच के लिए मिट्टी का नमूना बुवाई से कम से कम एक महीना पहले निकटतम मिट्टी जॉच प्रयोगशाला को भिजवा दें ताकि परीक्षण की रिपोर्ट आप तक बुवाई से पहले पहुंच जाय और आप सिफारिश के अनुसार खादों आदि का समय पर इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त कर सकें।
मिट्टी के नमूने की थेली पर ये सूचनायें अवश्य डालें।
-
1) किसान का नाम 2) खेत का खसरा नम्बर/पहचान, 3) दिनांक, 4) नमूने की गहराई 5) सिंचित या असिंचित 6) पिछली फसल कौन सी थी तथा कौन सी फसल बोना चाहते हैं, इत्यादि।
-
मिट्टी जॉच प्रयोगशाला से प्रत्येक नमूने के लिए अलग-अलग रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व के आधार पर सब्जी फसलों के लिए संस्तुत दर पर ही खाद व रसायनों का इस्तेमाल करें।
नमूना लेते समय सावधानियाँ
नमूना लेते समय हमें कुछ सावधानियॉ बरतनी आवश्यक हैं।
-
मिट्टी का नमूना खेत के उन्हीं स्थानों से लेना चाहिए, जो खेत का सही प्रतिनिधित्व करते हों।
-
खाद के ढेर, खेत की मेड़ या सिंचाई की नाली के नजदीक से नमूना कभी न लें।
-
खेत में उगे किसी पेड़ के जड़ वाले क्षेत्र से भी नमूना न लें।
-
उस स्थानों से नमूना न लें जहाँ पर खाद, चूना या कोई अन्य भूमि सुधारक रसायन तत्काल इस्तेमाल किया गया हो।
-
ऊसर आदि की समस्या से ग्रस्त खेत या उसके किसी भाग का नमूना अलग से लें और उसे अलग से प्रयोगशाला में भेजें।
-
जहाँ तक सम्भव हो, गीली मिट्टी का नमूना न लें।
-
उसे छाया में सुखाकर ही प्रयोगशाला में भेजें। धूप में सुखाने से उसमें उपस्थित पोषक तत्वों में आवांछिनीय परिवर्तन होने की संभावना रहती हैं।
-
नमूनों को खाद के बोरों, टे्रक्टर की बैट्री या किसी अन्य रसायन आदि से दूर रखें।
|
विद्युत चालकता (1: 2 के अनुपात में) की व्याख्या |
|||
|
विद्युत चालकता |
1.0 से कम |
1.0-2.0 |
2.0 से अधिक |
|
व्याख्या |
सामान्य मिट्टी, किसी भी फसल के लिए उपयुक्त |
सीमांत लवणीणता है, फसलों के बीज अंकुरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं |
अत्यधिक लवणीय है, फसलों के लिए हानिकारक हो सकते हैं |
|
सिफारिशें |
कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है |
भारी मिट्टियों में सुधार की आवश्यकता हो सकती है (हल्की मिट्टी में वांछनीय) |
भारी मिट्टियों में निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है। विशेष रूप से जब संवेदनशील व अर्ध-लवण – सहनशील फसलें उगानी हों। |
|
मिट्टी अभिक्रिया ;1:2 के अनुपात में) की व्याख्या |
||||||||
|
अभिक्रिया |
6.0 से कम |
6.0-8.5 |
8.6-9.0 |
9.0 से अधिक |
||||
|
व्याख्या |
अम्लीय मिट्टी है, कुछ फसलों के लिए अनुपयुक्त हो सकती है |
सभी फसलों के लिए उपयुक्त है |
क्षारीय है, कुछ फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है |
अत्यधिक क्षारीय हैं, फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है |
||||
|
सिफारिशें |
चूना व कार्बनिक खादों से सुधार की आवश्यकता होगी । |
कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है |
भारी मिट्टियों में सुधार की आवश्यकता होगी । हल्की मिट्टी में वांछनीय। इसके लिए जिप्सम व कार्बनिक खादों के उपयोग की आवश्यकता है। |
मिट्टियों में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता होगी । जिसके लिए जिप्सम, हरी खाद व कार्बनिक खादों का उपयोग किया जाना चाहिए। |
||||
|
मिट्टी उर्वरा (प्राथमिक तत्वों) की व्याख्या |
||||||||
|
मिट्टी उर्वरा |
जैविक कार्बन(प्रतिशत) |
उपलब्ध पोषक तत्व (कि.ग्रा./है.) |
व्याख्या |
|||||
|
नाइट्रोजन |
फास्फोरस |
पोटाश |
||||||
|
निम्न |
0.50 से कम |
280 से कम |
11 से कम |
120 से कम |
पोषक तत्वों की कमी |
|||
|
मध्यम |
0.5-0.75 |
280-560 |
11-25 |
120-280 |
पोषक तत्व सामान्य है |
|||
|
उच्च |
0.75 से अधिक |
560 से अधिक |
25 से अधिक |
280 से अधिक |
पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक है |
|||
|
गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्तर नीचे दिए गए मापदंडों से कम होने पर संबंधित उर्वरक के इस्तेमाल की आवश्यकता हैं। |
||||||||
|
पोषक तत्व |
मिट्टी में कमी के स्तर (मि.ग्रा./कि.ग्रा.) |
|||||||
|
गंधक |
10 |
|||||||
|
लोह |
4.5 |
|||||||
|
मैग्नीज |
2.0 |
|||||||
|
जस्ता |
0.6 |
|||||||
|
बोरोन |
0.5 |
|||||||
|
कॉपर |
0.2 |
|||||||
|
मॉलीब्डेनम |
0.1 |
|||||||
Authors:
श्री राकेश1, डॉ. एस. आर. भुनिया1, नारायण राम गुर्जर2 एवं मांगी लाल जाट3
1-शस्य विज्ञान विभाग, कृषि महाविधालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर
2-आनुवंशिकी एंव पादप प्रजनन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
3-प्रसार शिक्षा विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश
Email: shrirakeshchoudhary108@gmail.com