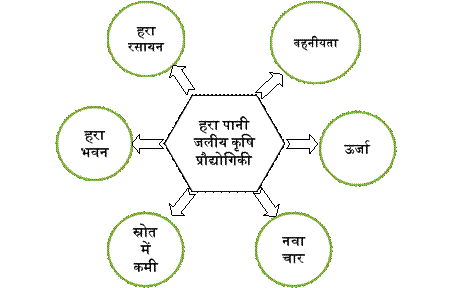25 Sep महासागरीय खेती: जल निकायों पर स्मार्ट और सतत कृषि
Ocean Farming: Smart and Sustainable agriculture on water bodies
कृषि एवं संबंधित उद्योग वैश्विक स्तर पर मौलिक और वास्तविक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम इस अपरिहार्य परिवर्तन को समझें और कृषि में संरचनात्मक बदलाव की वैश्विक गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कृषि में इस तरह के परिवर्तन के कारणों पर तीन बिन्दुओं के तहत चर्चा की जा सकती है।
सबसे पहले, विश्व में मानव आबादी की निरंतर वृद्धि वास्तव में हमें 2050 (संयुक्त राष्ट्र, 2019) तक 10 बिलियन जनसंख्या तक ले जायेगी और कोविड-19 जैसी महामारी ने पहले ही वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बहोत बडा व्यवधान पैदा किया है।
दूसरा, अंधाधुंध उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग, मीठे पानी का खनन, वनों की कटाई, भूमि क्षरण, मृदा की उर्वरता में गिरावट और अत्यधिक एकल फसल पध्दती इत्यादी से वैश्विक कृषि के कार्बन फुट प्रिंट बढ रहे है और उसके द्वारा संचालित वैश्विक जलवायु परिवर्तन इस बदलाव का कारण है।

तैरते कृषि का महासागरीय खेती के रूप में आभासी प्रतिनिधत्व (स्त्रोतः फोब्र्स पत्रिका 2020)
तीसरा, इस संरचनात्मक कृषि परिवर्तन को नैनो-उर्वरक, परिशुद्धि खेती, ऊध्र्वाधर खेती, ड्रोन, रोबोटिक्स, उपग्रह, स्वचालित कृषि मशीनरी और मशीन लर्निंग जैसी नवीन वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा भी संभव किया जा रहा है।
वर्तमान में, वैश्विक भूमि क्षेत्र का 11 प्रतिशत क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है । लेकीन यह कुल वैश्विक सतह क्षेत्र का केवल 3 प्रतिशत है। वैश्विक सतह क्षेत्र के 70 प्रतिशत क्षेत्र पर जहा परंपरागत कृषि उत्पादन नहीं किया जाता है वहा महासागरीय खेती एक विक्लप देता है।
महासागरीय खेती को वैज्ञानिक रूप से अपनाने से खादयान्न एवं पोषण सुरक्षा तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संबोधित कर सकते है। भारत की समुद्री तटरेखा 7516.6 किमी है जिसमें 5422.6 किमी मुख्य भूमि समुद्री तटरेखा तथा 1197 किमी भारत के द्वीप समूहों से घिरी है। यह तटरेखा भारत के 9 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में फैला है और इसमे 21.7 लाख किमी2 क्षेत्र, (जो कुल मुख्य भूमि क्षेत्र के 66 प्रतिशत के है) विशिष्ठ आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) है (सतीश और अन्य, 2018) ।
भारतीय तटीय क्षेत्र समृद्ध जैविक उत्पादकता और विविधता वाले हैं इसलिए हमेशा व्यापक मानवीय गतिविधियों के केन्द्र हैं। हिन्द महासागर की विभिन्न प्रजातियों की मछलिया, समुद्री खरपतवार और कई अन्य वनस्पतिया प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत है, जो सैकड़ों दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों में कच्चाी सामग्री का काम करता है ।
इसके अलावा हमारे पास कई बंदरगाह है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के केन्द्र हैं। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक तरीके से मछली पकड़ने के कारण हमारे मछली भंडार में कमी (1974 में 90 प्रतिशत से 2017 में 65 प्रतिशत) दर्ज की है।
इसलिए, हमारे महासागर से अन्य वैकल्पिक प्रोटीन स्त्रोतों का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है तथा हमारे गरीब मछुआरे समुदाय के पुनर्वास पर भी विचार करना चाहिए जो पूरी तरह से आय के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में मछली पालन पर निर्भर है।
कृत्रिम मछली पालन एक विकल्प है जिसे कई लोगों ने अपनाया है लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां है। इस प्रकार समुद्री खरपतवार और खाद्य हेलोफाइट संभावित वैकल्पिक स्थायी प्रोटीन स्त्रोतों के रूप में काम करते है।
भारत के समुद्र में वैकल्पिक प्रोटीन का प्रमुख स्त्रोत
समुद्री खरपतवार
समुद्री खरपतवार तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है जो विविध समुद्री जीवन को अमूल्य सहायता प्रदान करते है। इन समुद्री खरपतवारों का आर्थिक मूल्य तटीय क्षेत्रों के कम संसाधन वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। उनका उपयोग खादयान्न एवं चारा के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे प्राप्त होने वाले फाइकोकोलोइड महत्वपूर्ण निर्यात मूल्य हैं।
जैव ईंधन, न्यूट्राक्यूट्किल्स, दवाओं और खाद्य योज्य के रूप में उनके उपयोग के लिए उनकी व्यापक जांच की जाती है। भारत में समुद्री खरपतवारों की 844 प्रजातियां जिनमें से 366 प्रजातियां गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर पाई जाती हैं। अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में भारतीय समुद्री शैवाल उद्योग की विशिष्टता यह है कि यह फाइकोकोलाइड उत्पादन के लिए प्राकतिक रूप से उगी हुई फसल पर बहुत अधिक निर्भर करता है (गणेशन और अन्य 2019)।
गेलिडियाला सेरोसा और ग्रेसिलेरिया एडुलिस दो प्रमुख प्रजातियां हैं जिन्हें ऐगार उत्पादन के लिए काटा जाता है जबकि सारगेसम और टर्बिनेरिया जाति का एल्गिनेट उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। इसे कटाई के बाद समुद्र के किनारे सुखाया जाता है और औद्योगिक खरीदारों को आपूर्ति की जाती है।
सूखा गेलिडियाला को 1800 यूएस डाॅलर प्रति टन जबकि सारगेसम और टर्बिनेरिया जाति को 800 यूएस डाॅलर प्रति टन तक मिलता है। इस सफलता मॉडेल को ध्यान में रखते हुए, भारत की अत्यधिक समृद्ध तटीय रेखा पर अधिक से अधिक समुद्री खरपतवार प्रजातियों की खेती की जा सकती है। भारतीय तट क्षेत्रों में, दक्षिण-पूर्व समुद्री शैवाल की खेती के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें मध्यम तरंग क्रिया और नाइट्रोजन और फाॅस्फोरस के प्रचुर स्त्रोत के साथ समतल, उथला और चैड़ा तटीय तट हैं।
इसके अलावा, इन तटों में तापमान और लवणता की सीमा इष्टतम है, जो उन्हें मानसून के अलावा समुद्री खरपतवारों की साल भर की खेती के लिए आदर्श बनाती है। समुद्री खरपतवार की खेती के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल जैसे बांस, रस्सी और लंगर आधार भी इन स्थलों पर आसानी से उपलब्ध हैं। इसमें मछुआरे महिला समूह के लिए आजीविका स्त्रोत के रूप में भी उच्चतम क्षमता है जो अंततः इन मछुआरे परिवारों के बेहतर सामाजिक और आर्थिक निर्वाह की ओर ले जाएगी।
हेलोफाइट्स
भारत के समुद्र/तटीय क्षेत्रों से पादप प्रोटीन का एक अन्य संभावित स्त्रोत हैलोफाइट सैलिकोर्निया जाति है। यह आमतौर पर दलदल, समुद्री तटों और कीचड़ युक्त किनारों पर पाया जाता है। इसे आमतौर पर पूरे भारत में पिकलवीड, ग्लासर्वोट, समुद्री फलियां और समुद्री शतावरी के रूप में जाना जाता है। सैलिकोर्निया की कुछ प्र्रजातियां 3 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड स्तर सहन करके अपना जीवन चक्र पूरा कर सकती हैं।
भारत में, इस हेलोफाइट का उपयोग खाद्य फसल के साथ-साथ अखाद्य प्रयोजनों के लिए भी किया जाता रहा है। यह संयंत्र प्राचीन काल से कांच निर्माण के लिए सोडा का स्त्रोत था। पौधों से उत्पादित नमक का पहला स्त्रोत एक पत्ती रहित झाड़ी सालिकोर्निया ब्राचिआटा है और इसे 2003 मंे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) – केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई), गुजरात, भारत ने बनाया था।
सामान्य नमक के विपरीत इस वनस्पति के नमक में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के लवण होते हैं। प्रक्षेत्र परीक्षणों से पता चला है कि इसमें 3-4 टन वनस्पति नमक/हेक्टेयर उत्पादन करने की क्षमता है जो तटीय इलाकों के कम संसाधन वाले किसानों को 10-12 रूपये प्रति किलोग्राम का बाजार भाव पर दे सकते है। ’’सलोनी’’ नामक सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित नमक उत्पाद भी गुजरात में व्यावसायकि पैमाने पर विकसित किया गया था (झा और अन्य 2012)।
बीज में सोडियम की कम मात्रा इसे मधुमेह, अस्थमा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कैंसर के खिलाफ इसके अन्य औषधीय गुणों के अलावा मानव हृदय के लिए एक बहुत अच्छा स्त्रोत बनाती है।
इसके अलावा, इसके बीजों में खाद्य तेल पॉली अनसेच्युरेटेड फॅटी अॅसिड से भरपूर होता है और फॅटी अॅसिड प्रोफाइल में कुसुम के पौधे के समान होता है। इसका उपयोग भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में हरी सलाद के रूप में भी किया जाता है।
सैलिकोर्निया ब्राचीआटा की जीवाणुरोधी, क्षयरोधी और एंटीआक्सीडेंट गतिविधियां पहले बताई गई हैं। यह बहुत लोकप्रिय है और आमतौर पर पश्चिमी और पूर्वी तट के ग्रामीणों द्वारा जानवरों के चारे, हर्बल नमक और तेल के स्त्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि पूरे पौधे की राख को खुजली के उपचार में उपयोगी बताया गया है।
हाल ही में इसके पॉलीसेकेराइड और फेनोलिक यौगिकों, तेल, प्रोटीन, फ्लेवोनोइड्स, स्टेरॉल्स, सैपोनिन, अल्कलाइड और टैनिन के लिए अन्य फाइटोकेमिकल प्रोफाइल पर गहन अध्ययन चल रहा है और आशाजनक परिणाम दिखाता है। भारतीय प्रजाति सैलिकोर्निया ब्राचिआटा की ऑलिगोसेकेराइड प्रोफाइलिंग की गई और परिणामों से पता चला कि यह पौधा पूरक आहार का समृद्ध स्रोत है।
भारत के तटों पर इस पौधे की बड़े पैमाने पर खेती के पारिस्थितिक लाभों को बंजर लवणीय भूमि का उपयोग, हरित पट्टी के विस्तार, तटीय विकास और संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। अंत में, आर्थिक लाभ, विशाल निर्यात आय और निजी औद्योगिक और संस्थागत सहयोग इन असंख्य खूबियों को देखते हुए इस हेलोफाइट को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.आर.) के लिए गर्व की बात है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय मछली तकनीकी संस्थान का अनुमोदन किया गया है। अनुसंधान समूह ने प्रस्तावित किया कि समुद्री शैवाल से सल्फेटेड पॉली सेकेराइड कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली अणु हो सकता है, इसलिए सार्श कोव-2 (झा और अन्य 2020) के खिलाफ अध्ययन के लिए एक उम्मीदवार अणु है।
निरंतर समुद्री अन्वेशषण के साथ, समुद्र से बहुत अधिक वनस्पतियों की खोज की पूरी संभावना है जिन्हें परंपरागत रूप से अनदेखा किया गया था लेकिन अब खाद्य फसलों के रूप में आदर्श उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए, ऐसे संभावित पौधों की पहचान करना और उनकी व्यावसायिक आधार पर खेती करना भारतीय कृषि प्रणाली में नए रास्ते खोल सकती है। हालांकि, अवैज्ञानिक और अत्यधिक खेती को रोकने और पर्यावरणीय जीविका सुनिश्चत करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।
समुद्री सतह के नीचे कृषि
उद्गमियों के एक समूह ने अमेरिका में समुद्र की तल पर फसलों को खेती शुरू की है। इटली के एक स्कूबा डाइविंग कंपनी ने 2012 में ’’नेमो गार्डन प्रोजेक्ट’’ नामक एक परियोजना शुरू की और तब से वह समुद्र तल में विशेष संरचनाओं में तुलसी, स्ट्रॉबेरी, ऑर्किड और मसूर जैसी फसलों को उगाकर प्रयोग कर रही है।
इस संबंध में अमेरिका, कनाडा और इटली के विभिन्न अनुसंधान समूहों द्वारा विशेष उच्च अंत स्वायत्त जलीय कृषि उपकरण विकसित किए गए हैं, जिससे समुद्र की खेती की इस नई अवधारणा को परिभाषित करने में मदद मिली है। समुद्र की लवणीय स्थितियों के लिए चावल का परीक्षण तथा बार-बार आने वाले तूफानों को भी सहन कर सके ऐसी व्यवस्था विकसीत करने के प्रयोग चल रहे हैं ।
समुद्र में चावल की खेती की संभावना वैश्विक खाद्य संकट को संबोधित करने के दोहरे उद्धेश्य को पूरा करती है और ’’ब्लू कार्बन’’ के स्रोत के रूप में भी कार्य करती है क्योंकि यह वायुमंडलीय और समुद्री कार्बनडाई ऑक्साइड को अवशोषित करती है।
निष्कर्ष
समुद्री खेती का सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक लाभ ब्लू कार्बन का स्रोत है। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी मानवजनित कार्बन उत्सर्जन का एक तिहाई समुद्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल संतृप्ति के परिणामस्वरूप यह मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। बदले में, महासागर अधिक से अधिक अम्लीय होता जा रहा है, जो समुद्री जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
एक और चैंकाने वाला तथ्य यह है कि समुद्र के शीर्ष दस फीट में मौजूद गर्मी पूरे वातावरण से अधिक है। इसलिए, महासागरीय खेती जैसी नवीन तकनीकों में इस अतिरिक्त कार्बन को उत्पादक उद्धेश्यों के लिए सुरक्षित रूप से निकालकर हमारे महासागर को बचाने की अपार संभावनाएं हैं।
समुद्र पर ऐसी परियोजनाओं को लागू करते समय बहुत सावधान रहना होगा। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए और इनपुट के किसी भी प्रकार के रिसाव को रोकने के लिए सभी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कई समुद्री जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है।
हालांकि, इस तकनीक को मुख्यधारा लाने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। एक बात निश्चित है कि फ्लोटिंग क्राॅप आइलैंड्स और अपतटीय समुद्र के नीचे की खेती अत्यधिक नवीन है और इसमें भविष्य में अंतर्देशीय कृषि के पूरक होने की क्षमता है।
संदर्भ
- संयुक्त राष्ट्र, 2009, संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक और सामाजिक मामलों काविभाग, जनसंख्या प्रभाग। विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2019। यहां से उपलब्ध: https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/ [एक्सेस: 2020-08-20]
- सतीश एस, कंकारा आर एस, सेलवन एस सी, उमामहेश्वरी एम, रशीद के, 2018, वेव-बीच सेडिमेंट इंटरेक्शन विथ शोरलाइन चेंजेस अलंग ए हेडलैंड बाउंडेड पॉकेट बीच, भारत का पश्चिमी तट। पर्यावरण पृथ्वी विज्ञान। 77: 174-185।
- गणेशन एम, त्रिवेदी एन, गुप्ता वी, माधव एस, रेड्डी सी वी आर, लेविन आई.ए, 2019, भारत में समुद्री शैवाल संसाधन – विविधता और खेती की वर्तमान स्थिति: संभावनाएं और चुनौतियाँ। बोटानिका मरीना। 62: 463-482।
- झा बी, गोंटिया आई, हार्टमैन ए, 2012, हेलोफाइट सैलिकोर्निया ब्राचिआटा की जड़ें पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता वाले नए हेलोटोलेरेंट डायज़ोट्रॉफ़िक बैक्टीरिया का एक स्रोत हैं। पौधे और मिट्टी। 356: 265-277.
- झा ए के, मैथ्यू एस, रविशंकर सी एन, 2020, क्या समुद्री शैवाल से सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड्स COVID-19 महामारी के लिए रोगनिरोधी और/या चिकित्सीय समाधान प्रदान कर सकते हैं? वर्तमान विज्ञान। 119: 172-174।
लेखक
विनीत टी. वी1., रवीकिरण के. टी2., सागर द. विभुते1 एवं नवीन वर्मा2
1केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, भरूच
2केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ
ईमेल – vibhutesagar5@gmail.com