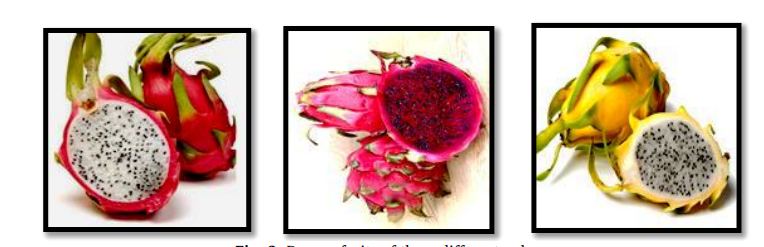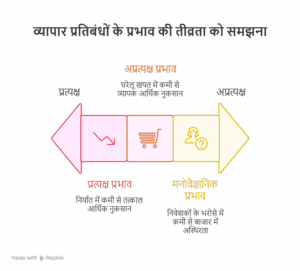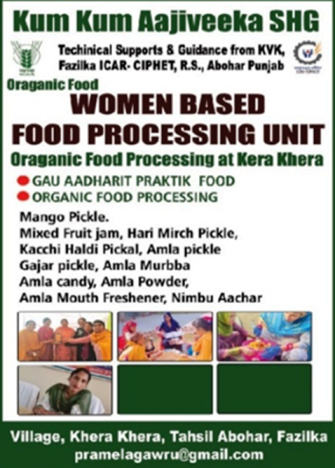09 May Relay Farming of Muskmelon in Wheat for higher Income
Under relay farming method, before the harvesting of base crop, the next crop is sown in the field in the standing condition of base crop and the subsequent crop is called Utera crop. With the use of relay farming, the farmer brother is able to harvest crops with limited resources (land, time, water, labor etc.) and less cost.
अधिक आय के लिए गेहूँ में खरबूज कि रिले खेती
सब्जियों का भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुत सी दूसरी फसलों की तुलना में प्रति ईकाई क्षेत्र में अधिक पैदावार देती है और कम समय में तैयार हो जाती है। भारत में खीरा वर्गीय कुल की लगभग 20 प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। इनमें धीया/ लौकी, तोरी, करेला, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कद्दू/ सीताफल, चप्पनकद्दृ, टिण्डा, परवल, फुट, आदि मुख्य है।
ये सभी बेलवाली फसलें होती हैं जो कम कैलोरी व सरलता से पचने वाली होने के साथ-साथ विटामिन्स, अमीनो अम्ल एवं खनिज लवणों का अच्छा स्त्रोत है।
उत्तर भारत के मैदानी भागो में साघारणत्या आलू, गाजर, मटर, सरसों, तोरिया आदि फसल लेने के उपरातं अधिकतर किसान भाई जनवरी के अंत से लेकर मार्च के प्रथम पखवाड़े तक खीरा-ककड़ी वर्गीय सब्जियों की बुवाई बीज द्वारा करते है तथा फसल की पैदावार अप्रैल से जून तक चलती है।
दिसंबर या जनवरी माह में पॉलीथीन घर में थैलियों में तैयार किये गए पौधों को फरवरी के अतं में (पाला पड़ने का खतरा समाप्त होने पर) रोप कर इन फसलों की अगेती फसल ली जाती है जबकि अप्रैल में गेहूँ की कटाई उपरांत इन सब्जियों (खरबूज, तरबूज, पेठा आदि) की बिजाई करने से, बरसात (जून माह में) के कारण फलों की गुणवत्ता में कमी आने से आर्थिक हानि होने की सम्भावना बनी रहती है।
प्रयोगों में पाया गया है कि गेहूँ में ककड़़ी-वर्गीय सब्जियों की अंतर-रिले फसल उत्पादन विधि के उपयोग से किसान भाई गेहूँ के खेत का उपयोग इन सब्जियों के फसल उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक कर सकते है। बहू-फसलीय कृषि के अंतर्गत रिले खेती फसल उत्पादन की एक परंपरागत एवं महत्वपूर्ण पद्धति है।
इस पद्धति में आघार फसल की कटाई से पहले आघार फसल की खड़ी अवस्था में ही खेत में अगली फसल की बुआई की जाती है तथा अनुवर्ती फसल उतेरा फसल कहलाती है। रिले खेती के उपयोग से किसान भाई सीमित संसाधनों (भूमि, समय, पानी, श्रम आदि) एवं कम लागत से फसल लेने में सक्षम होता है।
रिले फसल उत्पादन विधिः
रिले फसल उत्पादन की इस पद्धति में गेहूँ (आघार फसल) की बुवाई के समय ही खीरा-ककड़ी वर्गीय सब्जियों (उतेरा फसल) के लिए भी योजना बना ली जाती है। गेहूँ की बीजाई हेतु खेत तैयार करते समय 4.5 से 5 मीटर की दुरी पर 45 सै. मी. चौड़ी व 30-40 सै.मी. गहरी नालियां बना कर छोड़ देतें है। नालियों के बीच में गेहूँ की बीजाई की जाती है। गेहूँ की बीजाई (अक्टुबर-दिसंबर) से लेकर फरवरी तक इन नालियों को खाली रखते है।
इस अवधि के दौरान इन नालियों का उपयोग तोरीया, पालक, मेथी मूली, गाजर, मटर आदि अंतर-फसल उगाकर भी किया जा सकता है। अगर गेहूँ की बीजाई हेतु खेत तैयार करते समय नालियां नहीं बनाई गई हों तो जनवरी माह से मध्य फरवरी तक 4.5 से 5.0 मीटर की दुरी पर नालियां (6 से 8 नालियां प्रति एकड़) तैयार करते है। नालियों के किनारों पर 50-60 सै.मी. की दूरी पर थावले बना लेते है तथा नालियों को खरपतवार रहित कर लिया जाता है।
नालियों में तैयार किए गए इन थावलों में मध्य फरवरी में (पाला पड़ने का खतरा समाप्त होने पर) बीज लगाते है। अगर बेल वर्गीय सब्जियों (खरबूज, तरबूज, पेठा, घिया, तोरी आदि) की पौध पॉलीथीन बैग में तैयार की गई है तो नालियों में पौध का रोपण गैहूं की कटाई से 45 से 60 दिन पहले करते है। पौध रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिचांई करना आवश्यक होता है।
पॉलीथीन बैग में पौध तैयार करने हेतु 15 से.मी. लम्बे तथा 10 से.मी. चौड़ाई वाले पॉलीथीन (100-200 गॉज) के थैलों में मिटटी, रेत व खाद का मिश्रण बनाकर भर लेते है। प्रत्येक पॉलीथीन बैग की तली में 4-5 छोटे छेद कर लिए जाते है तथा मिश्रण भरते समय यह घ्यान रखते है कि प्रत्येक पॉलीथीन बैग के किनारे पर 2-3 से.मी. जगह पानी देने के लिए खाली रहे। इन थैलों में बीज बोने से पहले बीज को फफुंदी नाशक से उपचारित कर लें।
प्रत्येक थैले में 2-3 उपचारित बीज दिसम्बर-जनवरी माह में लगाए जाते है। बीजों की बुवाई के बाद थैलों में हल्की सिचांई फव्वारे की मदद से करते है। बीज अंकुरित होने पर प्रत्येक थैले में एक स्वस्थ पौधा छोड़कर बाकी पौधे निकाल देते है। पॉलीथीन बैग में तैयार किये जाने वाले पौधों को ठंड से बचाने हेतु आवश्यकतानूसार पॉलीथीन घर का प्रयोग किया जाता है।
खेत में पौधे लगाने की इस विधि में खाद व उर्वरकों का प्रयोग, निराई-गुड़ाई व सिंचाई आदि क्रियाएं नालियों के अंदर ही की जाती है। इस विधि में नालियों के बीच की जगह में सिंचाई नहीं की जाती जिससे फल गीली मिट्टी के सम्पर्क में नहीं आते तथा खराब होने से बच जाते है।
रिले फसल उत्पादन से लाभ :
इस विधि को अपनाने से गेहूँ–धान फसल चक्र प्रणाली वाले क्षेत्रों में गेहूँ कटाई के बाद तथा धान की रोपाई तक (अप्रैल से जून) किसान भाई खेत का उपयोग खरबूज, लौकी, तोरी, तरबूज, कद्दू/सीताफल, पेठा आदि (जिनकी बेल अधिक फेलती है) सब्जियों के फसल उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक कर सकते है।
गैहूं में ककड़ी वर्गीय सब्जियों की रिले फसल उत्पादन विधि का उपयोग करने से (15 जून तक) खरबूज, तरबुज, धीया व पेठा में क्रमशः 200, 300, 250 एवं 350 किव्ंटल प्रति हैक्टेयर फलों की पैदावार होती है जबकि गैहूं कटाई के उपरांत मूंग उगाने पर 10 किव्ंटल (बीज) एवं व लोबिया उगाने पर 30 से 35 किव्ंटल (फलिंया) प्रति हैक्टेयर की दर से प्राप्त होती है।
धान-गैहूं फसल प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न फसलों के आर्थिक विशलेषण में पाया गया कि धान-गैहूं, धान-गैहूं-मूंग, धान-गैहूं-लोबिया व धान-गैहूं-खरबूज फसल चक्र से क्रमशः 1.80, 2.20, 2.52 तथा 3.64 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से सकल आय प्राप्त हुई तथा धान-गैहूं, धान-गैहूं-मूंग, धान-गैहूं-लोबिया व धान-गैहूं-खरबूज फसल चक्र से क्रमशः 137, 167, 191 तथा 276 किव्ंटल प्रति हैक्टेयर गैहूं समतुल्य पैदावार प्राप्त हुई।
सारणी-1: कद्दूवर्गीय सब्जियों में बीज दर, फलों एवं बीज की पैदावार
|
फसल |
बीज दर (किलो प्रति एकड़) |
फलों की औसत पैदावार (क्वि. प्रति एकड़) |
बीज की औसत पैदावार (किलो प्रति एकड़ ) |
|
तरबुज |
1.5-2.0 |
120-150 |
75-80 |
|
पेठा |
1.5-2.0 |
120-150 |
100-150 |
|
खरबूज |
0.75-1.0 |
60-80 |
60-70 |
|
धीया /लौकी |
1.5.2.0 |
100-120 |
150-200 |
सारणी-2: कद्दूवर्गीय सब्जियों के प्रमुख कीट एवं रोग तथा उनके नियंत्रण के उपाय
|
कीट/रोग |
हानि के लक्षण |
निंयत्रण |
|
माहू या चेपा |
इस कीट के निम्फ व व्यस्क तने, कोमल पत्तियों व पुष्पकलिकाओं से रस चुसते है। |
ईमिडाक्लोपरिड 17.8 एस.एल. या थायोमिथेक्साम 70 डब्लू.एस. 0.5-0.70 मि0लि0 दवा प्रति लिटर पानी की दर से छिड़काव करें। |
|
लीफ माइनर |
यह कीट पत्तियों के उपरी भाग पर टेढी-मेढी भूरे रंग की सुरंग बनाता है तथा इसका लारवा पत्तियों को हानि पहुंचाता है। |
|
|
सफेद मक्खी |
इसका प्रकोप पत्तों की निचली सतह पर शिराओं के बीच में होता है। यह कीट पत्तियों से रस चुसता है। इसके प्रभाव से पत्तियां पीली हो जाती है तथा पत्ते सिकुडकर नीचे की तरफ मुड जाते है। सफेद मक्खी विषाणु रोग का प्रसार भी करती हे। |
|
|
फल भेदक मक्खी |
फल भेदक मक्खी का प्रकोप फरवरी से लेकर नवंबर तक होता हें। मादा मक्खी अपने अंड रोपक से कोमल फलों के गूदे में अंडे देती हे। मैगट फलों के अंदर गूदे को खाकर नष्ट कर देता है। |
डाइमिथोएट 30ई0 सी0 अथवा मेलाथियान 50ई0सी0 अथवा मिथाइल डेमेटोन 25ई0सी0 1-1.5 मि0लि0 दवा प्रति लिटर पानी की दर से छिड़काव करें। |
|
लाल कद्दू भृंग |
इस कीट के ग्रब (प्यूपा) छोटे पौधों के तनों में जमीन के पास से छेद कर देते हैं जिससे पौधा सूख जाता है। ये ग्रब (प्यूपा) जमीन पर रखे फलों के निचले भाग में छेद कर फलों को हानि पहुंचाते है। भृंग (व्यस्क) पौधों की पत्तियों व फूलों को खाकर नष्ट करता है। |
|
|
तना विगलन/ कॉलर रोट |
भूमि की सतह के पास पौधों के तनों पर भूरे रंग के पनीले तथा नरम धब्बे बनते है। पौधे पीले पड़कर सूख जाते है। |
ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम अथवा कार्बाडांजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। |
|
चूर्णी फफूंद |
इसके लक्षण पत्तियों व तनों की सतह पर सफेद या धुंधले धूसर सुक्ष्म आभा युक्त धब्बों के रूप प्रगट होते है जो बाद में सफेद चूर्ण के रूप में फैल जाते है। |
10-15 दिन के अंतर पर कैराथेन के 0.05 प्रतिशत के धोल का छिड़काव करें। |
|
एर्न्थेक्नोज |
आरंभ में इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों, तने व डटंलों पर छोटे पीले या जलाभ् धब्बे दिखाई देते है जो बाद में मिलकर बड़े हो जाते है। फलों पर गोल सिकुड़े हुए जलाभ् धब्बे बन जाते है। |
मैंकोजैब या कार्बाडांजिम के 0.20 प्रतिशत के धोल का छिड़काव करें। |
Authors:
सुरेश चंद राणा, पी.बी. सिंह एवं विनोद कुमार पंडिता
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल
Email: sureshiariknl@gmail.com
Related Posts
………………………………………
Related Posts