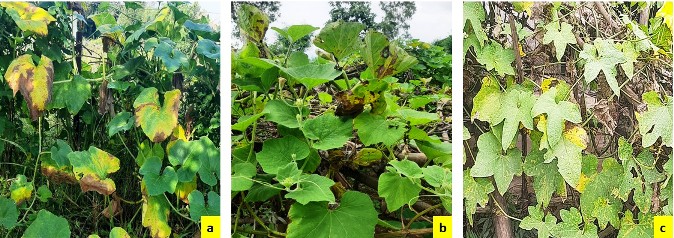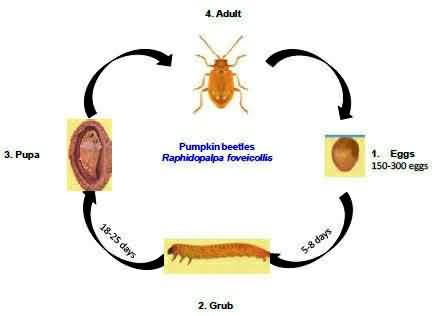14 Mar सीताफल में संकर बीज उत्पादन की तकनीक
Posted at 08:48h
in Seed production
Hybrid seed production technique of Pumpkin
पुष्प जैविकी:
सीताफल में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग-अलग जगह पर लगते हैं। फूल बडे आकार के तथा चमकीले पीले रंग के होते हैं। मादा पुष्प आकार में नर पुष्पों से बडे होते हैं। मादा फूल छोटी डंडी एवं नीचले भाग में फल आकृति लिए होते हैं।


नर पुष्पों की डंडी लम्बी होती है। पौधों में प्राय नर फूल पहले आते हैं तथा बाद में मादा एवं नर पुष्प मिश्रित रूप से आते हैं। फूल प्रात: काल में 5 से 7 बजे के बीच खिलते हैं और 12 बजे दोपहर तक खिले रहकर दोपहर बाद बंद हो जाते हैं। पुष्प खिलने के समय नर पुष्प में अत्यिधिक जीवित परागण मिलते हैं तथा मादा फूल में वर्तिकाग्र भी निषेचन के लिए अधिकतम ग्राही होता है। परागण का कार्य प्रात: काल 7 बजे से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए क्योकि समय बीतने पर परागण चिपचिपा और गीला हो जाता है। मकरन्द ग्रन्थियां मादा पुष्पों में नर पुष्पों की अपेक्षा अधिक होती हैं। परागण कार्य कीटों जैसे मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है।
खेत का चुनावः
संकर बीज उत्पादन के लिए खेत समतल, उपजाऊ एवं खरपतवार रहित होना चाहिए तथा उसमें समुचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की मिटटी का पीएच मान 6.5-7.5 के बीच उपयुक्त रहता है। खेत में सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
मौसम का चुनाव:
सीताफल के संकर बीज उत्पादन के लिए ग्रीष्म ऋतु उपचुक्त होती है। पोली हाऊस में जनवरी में बीज बुआई करके फरवरी के पहले सप्ताह में पोध रोपाई की जाती है।
खाद एवं उर्वरक:
एक किलोग्राम गोबर की सडी खाद, 50 ग्राम डी.ए.पी. तथा 25 ग्राम एम.ओ.पी.प्रति थमला (हिल) बुआई से 5-7 दिन पहले मिलाना चाहिए। 50 ग्राम यूरिया प्रति थमला, पौधों के 30-35 दिन के होने पर, देना चाहिए। नत्रजन की अधिक मात्रा देने से बचना चाहिए अन्यथा पौधों की वनस्पतिक बढवार अधिक होगी और परिणाम स्वरूप फलन प्रभावित होगा। 1% यूरिया या डी.ए.पी.के घोल का छिडकाव फल विकसित होते समय करने से फल अधिक संख्या में तथा अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। छिडकाव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।
पृथक्करण दूरी:
सीताफल एक पर-परागित (cross polinated) एवं उभयलिंगाश्री (नर व मादा पुष्प का एक ही पौधे के अलग अलग भागों पर आना) फसल है। आनुवांशिक रूप से शुद्व बीज उत्पादन के लिए, बीज फसल, अन्य किस्मों तथा व्यावसायिक संकर किस्मों के बीच में न्यूनतम 1000 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नर व मादा पैतृकों की बुवाई अलग-अलग खण्डों में न्यूनतम 5 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। पृथक्करण दूरी के अन्दर अन्य कद्दू वर्गीय फसलों जैसे चप्पन कद्दू एवं विन्टर स्कैवेश नही उगानी चाहिए।
बीज का स्रोत:
संकर बीज उत्पादन के लिए पैतृक जननों (Parents) का आधारीय बीज (Foundation seed)ही प्रयोग किया जाता है जिसे सम्बन्धित अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।
बीज दर व पौधअंतरण:
एक हैक्टेयर के लिए 2 कि.ग्रा. बीज (मादा पैतृक का 1.5 किग्रा तथा नर पैतृक का 0.5किग्रा) पर्याप्त होता है। यदि अंकुरण अधिक हो तो बीज की मात्रा घटाई जा सकती है। निरीक्षण व परागण की सुविधा के लिए दो सिंचाई नालियों के बीच की दूरी 4 मीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1.0 मीटर पर्याप्त रहती है।
बीज की बुवाई:
कद्दू जातीय सभी फसलों में बीज अंकुरण के लिए, दिन-रात का औसत तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच होना आवश्यक है। बीजों को बुवाई के 18-24 घंटे पुर्व उपचारित अवश्य करें। उपचारित करने के लिए, 2 ग्राम थीराम या कैप्टान प्रति किग्रा बीज के हिसाब से कुल बीज की मात्रा के बराबर पानी में घोल बनाकर,नर व मादा बीजों को चिन्हित करके भिगोदें। बुवाई से पूर्व बीजों को छाया में फैलाकर सुखा दें। सीताफल की बुआई खेत में सीधे बीज बुआई करके या पोलीहाऊस में पौध तैयार करके बाद में खेत में रोपाई करके की जाती है।
सीधे बीज बुआई विधि में प्रति हिल दो बीजों की, 2-3 इंच गहराई में बुआई करते हैं। बुआई के 15 दिनो बाद 2-4 पत्तियां आने पर अतिरिक्त पौधों को निकाल देना चाहिए तथा प्रति हिल एक पौधा रखना चाहिए। उत्तर भारत में अंकुरण के उपयुक्त तापमान 15 फरवरी के बाद ही आता है इसलिए इस विधि से बुआई करने पर फूल आने के समय तापमान बहुत अधिक हो जाता है जिससे नर फूल अधिक बनते हैं। साथ ही परागण में सहायक कीट भी अधिक ताप के कारण कम हो जाते हैं और फसल पैदावार तथा गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पडता है।
संकर बीज उत्पादन के लिए पोध तैयार करने की विधि ही उपयुक्त रहती है। जनवरी के प्रथम सप्ताह मे स्थाई या अस्थाई पोलिहाऊस में प्लास्टिक की थैलियों में मिट्टी भरकर बीज बुआई करते हें ।फरवरी के पैहल सप्ताह में तैयार पोध को खेत में रोपाई कर दी जाती है। इस विधि से बुआई करने पर फूल बनते समय तापमान बहुत अनुकूल होता है मादा फूल अधिक आते हैं तथा उस समय परागण करने वाले कीट भी अधिक होने से फसल अच्छी होती है।
नर-मादा पैतृकों का अनुपात तथा बुवाई विधि:
संकर बीज उत्पादन फसल के लिए पैतृकों की बुआई मुख्यत: दो विधियों से की जाती है।
एक खण्ड विधि: इस विधि में मादा तथा नर पैतृको मे रोपाई/बुवाई अनुपात 3:1 रखना चाहिए। पहले एक थमला नर बीज द्वारा तथा फिर 3 थमलें मादा बीज या पोध रोपाई द्वारा बोए जाते हैं। फिर इसी क्रम को बार बार दोहराया जाता है। नर पैतृक के पौधों को लकडी के डंडों या खुट्टियों से चिन्हित करें। नर तथा मादा पैतृको की बुआई या रोपाई के लिए अलग अलग श्रमिकों को लगाना अच्छा होता है।
प्रथक खण्ड विधि: इस विधि में मादा एवं नर पैतृकों की रोपाई/बुवाई अलग अलग खण्डों में एक ही दिन की जाती है। इसलिए कुल क्षेत्र के एक चौथाई भाग (1/4 भाग) को नर पौधों के लिए तथा तीन चौथाई (3/4) भाग को मादा पौधो के लिए चिन्हित कर लें। नर भाग में नर पैतृक की पोदो की रोपाई प्रत्येक हिल पर एक पोद के हिसाब से कर दें। इसी प्रकार मादा खंड में मादा पैतृको की हिल में बुआई करें
सिचांई :
सिचाई खुले खेत में पौधों की आवश्यकतानुसार दी जाती है। ध्यान रक्खें की पौधों में मुरझाने की अवस्था ना हाने पाये। सिचाईं सुबह 11 बजे से पहले या शाम का 4 बजे के बाद में ही करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए दो तीन निराई पर्याप्त रहती हैं।
रोगिंग :
नर और मादा खण्डों से अवांछित पौधों को पूर्ण रूप से समय समय पर निकालना चाहिए। पहली बार पुष्पन से पूर्व, दो बार पुष्पन व फल बनने की अवस्था में तथा अंतिम बार फलों के पकने या तुडाई के पूर्व जातीय लक्षणों के आधार पर निकालें। अवांछनीय पौधों, विषाणु सुग्राही और रोग ग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। अवांछनीय पौधों की संख्या कभी भी 0.05% से अधिक नही होनी चाहिए। फलों को तोडने के बाद बीज निकालने से पहले अल्प विकसित फलों को भी हटा देना चाहिए।
परागण प्रबंधन:
परागण की दो विधियां है हस्थ परागण व प्राकृतिक परागण। बीज उत्पादन फसल में हस्थ परागण प्राकृतिक परागण से अधिक अच्छा होता है।
प्राकृतिक परागण: मादा पैतृक में स्वनिषेचन को रोकने के लिए, पुष्पन से पहले ही नर कलिकाओं को मादा पैतृक पौधों से तोडकर नष्ट किया जाता है। यह कार्य बहुत ही सावधानी के साथ 45 दिन तक प्रत्येक दिन किया जाता है। पुष्पन होने पहले मादा व नर पुष्पों को सफेद रंग के बटर पेपर से ढक दिया जाता है। साथ साथ नर पैतृक पौधों से अल्प विकसित फलों को तोडते रहते हैं। इससे अधिक संख्या में नर फूल मिलते है। इस विधि में परागण कार्य कीटों विशेषकर मधुमक्खियों द्वारा होता है अत:कीटनाशकों का छिडकाव मधुमक्खियों के भ्रमण को ध्यान में रखकर करना चाहिए।


हस्थ परागण: इस विधि में मादा पैतृक के पौधों से नर पुष्प कलिकाओं कों खिलने से पहले ही तोडकर नष्ट कर दिया जाता है मादा पैतृक के पौधों से नर कलियां तोडने की प्रक्रिया 40-45 दिनों तक प्रतिदिन की जाती है।



मादा पैतृक पौधों में मादा पुष्पों को खिलने के एक दिन पूर्व यानि पहले दिन शाम के समय विशेष प्रकार के मोटे धागे से बांध दिया जाता है। उसी दिन नर पैतृक में नर पुष्पो को भी धागे से बांध दिया जाता है। अगले दिन सूर्य उदय होने के पहले या अधिकतम 7 बजे तक नर पुष्पों को तोडकर एकत्रित कर लिया जाता है तथा पुमंगों को वार्तिकाग्र के ऊपर धीरे धीरे रगडा जाता है। परागण का कार्य को देर से करने पर नर पुष्प के परागकोष में परागण गीले हो जाते हैं जिससे परागण क्रिया बाधित होती है। हस्त परागण के बाद पुन:मादा पुष्पदलों को धागे से बांध दिया जाता है तथा परागित फूल को पहचान के लिए टैग लगा देते हैं और उसपर परागण तिथि भी लिख दें। परागण कार्य प्रतिदिन सुबह 7 बजे से पहले, 40-45 दिनों तक किया जाता है।

सीताफल में परागण विधि का बीज उपज पर प्रभाव निम्न तालिका में दर्शाया गया है।
| विवरण | प्राकृतिक परागण | हस्त परागण |
| फलो की संख्या/पौधा(45दिन) | 1.78 | 3.27 |
| परिपक्व फल/पौधा | 1.05 | 1.63 |
| बीज उपज/पौधा(ग्रा.) | 46.00 | 83.66 |
| बीज उपज/फल(ग्रा.) | 44.08 | 52.33 |
| बीजों की संख्या/फल | 345.33 | 392.41 |
| भरे बीजों की संख्या/फल | 298.41 | 356.83 |
| खाली बीजों की संख्या/फल | 46.91 | 35.58 |
| 1000 बीजों का भार(ग्रा.) | 134.9 | 148.08 |
फलों का पकाना, बीज निकालना तथा सुखाना :
बीजों का पक्कवन फल सामान्यत:परागण के 70-85 दिन बाद तुडाई के योग्य हो जातें हैं। इस समय फल हरे रंग से सुनहरी पीले रंग के हो जाते हैं। फलों की तुडाई 2-3 बार में करना उत्तम रहता है। फलों के अधिक पकने पर खेत में सड कर नष्ट होने की संभावना रहती है।
कद्दू जातीय सब्जी फसलों का संकर बीज उत्पादन प्राय कम क्षेत्र (0.25-0.5एकड)में ही किया जाता है। इसलिए बीज निकालने का कार्य हाथो द्वारा ही किया जाता है। फलों का चाकू की सहायता से दो भागों में काटकर बीजों को रेशों से अलग निकाला जाता है। फिर बीजों को स्वच्छ बहते हुए पानी में धोया जाता है जिससे हल्के अविकसित बीज आसानी से अलग हो जाते हैं।
धोने के बाद बीजों को सीमेंन्ट के फर्श या तिरपाल क ऊपर सुखाया जाता है। रेशों से बीज आसानी से अलग हो इसके लिए फलों को 6-8 दिनों के लिए हवायुकत छायादार सुरक्षित स्थान पर रखकर सुखाना चाहिए। बीजो को एक दिन के लिए छाया में तथा बाद में तेज धूप या कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है। शुरू में 38 से 41 डिग्री तापक्रम में सुखाया जाता है तथा बाद में 32 से 35 डिग्री मे रखा जाता है। बीज तब तक सुखाया जाता है जबतक नमी की मात्रा 7% नही पहुचं जाती। वातीय दबाव पैकिगं के लिए बीजों में नमी की मात्रा 6% तक होनी चाहिए।
बीज उपज:
बीज उपज परागण विधि, फसल प्रबन्धन, प्रति पौधा फलो की संख्या तथा फलों के विकास से बहुत प्रभावित होती है। बीज उपज प्रति फल 44.08 ग्रा से 52.33 ग्रा. तथा औसत बीज उपज प्रति पौधा 83.66 ग्रा. होती है। पूसा संकर-1 के 1000 बीजों का भार प्राकृतिक परागण से 134.09 ग्रा. तथा हस्त परागण से 148.08 ग्रा. होता है।
Authors:
डा.बी.एस. तोमर एवं लोकेन्द्र सिहं
बीज उत्पादन ईकाई, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली,
ईमेल:bst_spu_iari@rediffmail.com
Related Posts
Bacterial leaf spot disease and prevention in pumpkin crops
कद्दू वर्गीय...
कृषि फसलों के बीज उत्पादन क्षेत्र का चयन एवं प्रबंधन
Seed...
8 Major insects and diseases of cucurbits and their control measures
कद्दू...
चने का फाउंडेशन और प्रमाणित बीज उत्पादन करने की तकनीक
Gram...
गेंहूं का बीज उत्पादन
The production of wheat crop for seed...
गेंहू के व्यवसायिक संकर बीज उत्पादन के लिए गेहूं में...